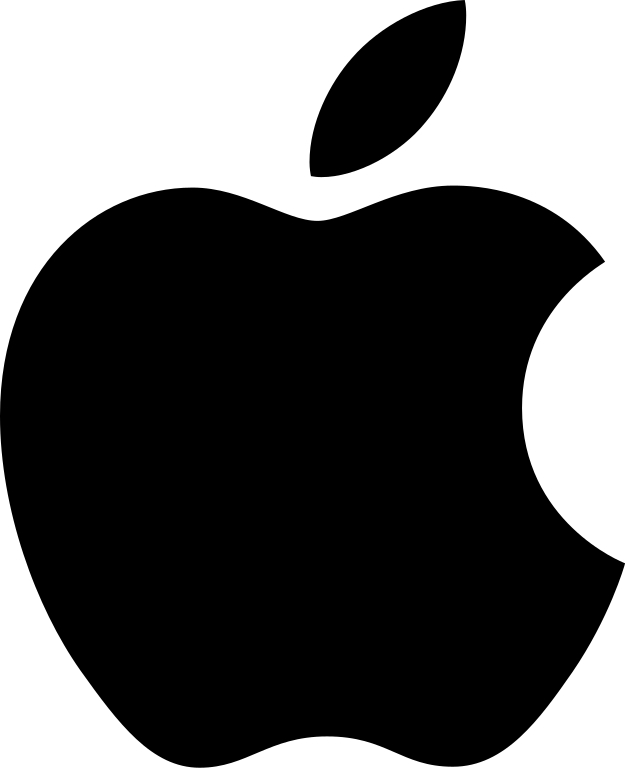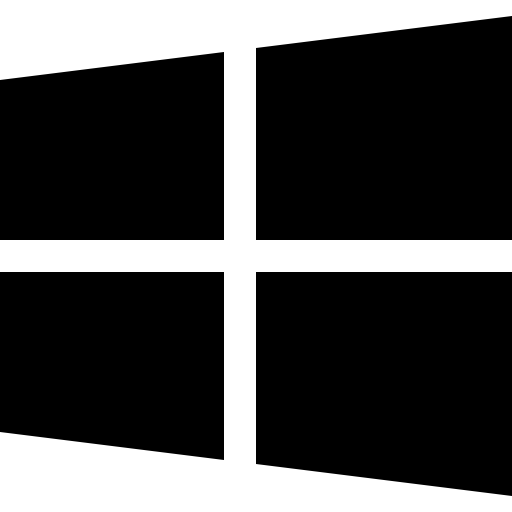एलपीजी सुधार: भारतीय अर्थव्यवस्था का कायापलट
भारत ने शुरू में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था। 1990 के दशक की शुरुआत में भारत में आर्थिक और वित्तीय संकट से निपटने के लिए उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण (एलपीजी) सुधारों को पेश किया गया था।
भारत ने विश्व बैंक के रूप में लोकप्रिय अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (IBRD) और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) से संपर्क किया, और संकट को प्रबंधित करने के लिए 7 बिलियन डॉलर का ऋण प्राप्त किया।
भुगतान संतुलन संकट के कारण:
- कमजोर राजकोषीय स्थिति: 1990 और 1991 में, राजकोषीय घाटा GDP का लगभग 8.4% था।
- तेल की कीमतें: 1990 और 1991 में कुवैत पर इराकी आक्रमण के कारण खाड़ी युद्ध ने तेल की कीमतों में तेजी ला दी।
- मुद्रास्फीति में भारी वृद्धि: परिवर्तन 6.7% से 16.7% तक हुआ, जो मुद्रा आपूर्ति में तेजी से वृद्धि के कारण था।
- सरकारी आंतरिक ऋण में वृद्धि: उच्च राजकोषीय घाटे के कारण सरकार का आंतरिक ऋण आसमान छू गया। यह 1985-86 में GDP का 35% से बढ़कर सभी रिकॉर्ड खर्च के स्तर पर 53% GDP के चौंकाने वाले आंकड़े पर पहुँच गया।
- विदेशी मुद्रा भंडार का ह्रास: भारत के पास विदेशी मुद्रा भंडार 1 बिलियन डॉलर से कम था।
- पूंजी पलायन: बिगड़ती आर्थिक स्थिति ने निवेशकों को भारत से अपनी पूंजी वापस लेने के लिए डर दिया। इसने संकट को और बढ़ा दिया और आर्थिक गिरावट का कारण बना।
नई आर्थिक नीति, 1991 को अपनाना:
संकट के जवाब में, भारत सरकार ने 1991 में नई आर्थिक नीति की घोषणा की, जो एलपीजी सुधारों (उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण) के रूप में जाने जाने वाले आर्थिक सुधारों की नींव थी।
- औद्योगिक नीति का उदारीकरण: उदारीकृत आर्थिक व्यवस्था में, आयात शुल्क कम या समाप्त कर दिए गए हैं। लाइसेंस परमिट राज (प्रतिबंधात्मक औद्योगिक लाइसेंसिंग) का अंत हो गया है और औद्योगिक विकास और प्रतिस्पर्धा में योगदान देने के उद्देश्य से अन्य विभिन्न अग्रणी उपाय किए गए हैं।
- निजीकरण कार्यक्रम: बाजार विनियमन, बैंकिंग क्षेत्र सुधार और दक्षता बढ़ाने के संबंध में निजी भागीदारी की सुविधा के लिए अन्य कदम।
- वैश्वीकरण: विनिमय दरों में बदलाव, व्यापार और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीतियों का उदारीकरण और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए अनिवार्य परिवर्तनीयता को हटाना।
उदारीकरण:
उदारीकरण के उद्देश्य:
- घरेलू उद्योगों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ाना।
- आयात और निर्यात को विनियमित करना जो विभिन्न देशों के साथ विदेशी व्यापार को प्रोत्साहित कर सके।
- विदेशी पूंजी और प्रौद्योगिकी को बढ़ाना।
- देश की वैश्विक बाजार सीमाओं का विस्तार करना।
- देश को ऋण से मुक्त करना।
प्रभाव:
- औद्योगिक क्षेत्र का विनियमन:
- 1991 से पहले: व्यापक औद्योगिक लाइसेंसिंग, सीमित निजी क्षेत्र की भागीदारी, लघु उद्योगों के लिए आरक्षण और मूल्य नियंत्रण/वितरण जैसे कड़े नियम।
- औद्योगिक लाइसेंसिंग: 9 उद्योगों (शराब, औद्योगिक विस्फोटक और रसायन, सड़क परिवहन) को छोड़कर सभी में समाप्त कर दिया गया, जिन्हें सरकार के अधीन रखा गया।
- लघु उद्योगों से वस्तुओं को प्रतिबंध मुक्त: इसने अधिकांश कीमतों को नियंत्रण मुक्त कर दिया।
- 1991 से पहले: व्यापक औद्योगिक लाइसेंसिंग, सीमित निजी क्षेत्र की भागीदारी, लघु उद्योगों के लिए आरक्षण और मूल्य नियंत्रण/वितरण जैसे कड़े नियम।
- वित्तीय क्षेत्र सुधार:
- वित्तीय क्षेत्र का विनियमन: 1991 से पहले की अवधि में RBI द्वारा व्यापक विनियमन देखा गया, जो वाणिज्यिक बैंकों, निवेश बैंकों (विकास वित्तीय संस्थानों), स्टॉक एक्सचेंजों और यहां तक कि विदेशी मुद्रा बाजार को विनियमित (या नियंत्रित) करने पर केंद्रित था।
- 1991 के बाद के सुधार: RBI को एक नियामक से सुविधाकर्ता के रूप में स्थानांतरित किया गया, जिससे वित्तीय क्षेत्र को निर्णय स्वायत्तता मिल गई।
- निजी क्षेत्र के बैंकों (भारतीय और विदेशी) की शुरुआत एफआईआई/एफडीआई के लिए उच्च सीमा (लगभग 74%) के साथ।
- वित्तीय क्षेत्र का विनियमन: 1991 से पहले की अवधि में RBI द्वारा व्यापक विनियमन देखा गया, जो वाणिज्यिक बैंकों, निवेश बैंकों (विकास वित्तीय संस्थानों), स्टॉक एक्सचेंजों और यहां तक कि विदेशी मुद्रा बाजार को विनियमित (या नियंत्रित) करने पर केंद्रित था।
- कर सुधार:
- 1991 के बाद कर सुधार: मुख्य रूप से राजकोषीय नीति, अर्थात सरकार की कराधान और सार्वजनिक व्यय नीतियों को बदलना।
- आय और निगम करों का निरसन; 1991 के बाद व्यक्तिगत आयकर और निगम कर की दरें कम रहीं।
- 1991 के बाद कर सुधार: मुख्य रूप से राजकोषीय नीति, अर्थात सरकार की कराधान और सार्वजनिक व्यय नीतियों को बदलना।
- अप्रत्यक्ष कर सुधार:
- वस्तुओं पर अप्रत्यक्ष करों को सुव्यवस्थित करने के लिए पहल।
- वस्तुओं के संबंध में एक आम व्यापार संघ बनाने की योजना बनाई गई।
- जीएसटी अधिनियम 2016: 2016 में प्रयास सार्थक हुए, जिससे वस्तु और सेवा कर अधिनियम
2016 के तहत व्यापक अप्रत्यक्ष कर प्रणाली लागू हुई। जुलाई 2017 से लागू, कर प्रशासन को सुचारू बनाने और चोरी को रोकने का इरादा है।
- वस्तुओं पर अप्रत्यक्ष करों को सुव्यवस्थित करने के लिए पहल।
- विदेशी मुद्रा सुधार: संकट को दूर करने के लिए रुपये का तत्काल अवमूल्यन, विदेशी मुद्रा प्रवाह को बढ़ावा देना।
- विनिमय दर सुधार:
- विदेशी मुद्रा की मांग और आपूर्ति के आधार पर, रुपये के मूल्य पर सरकारी नियंत्रण कम करना।
- विदेशी मुद्रा की मांग और आपूर्ति के आधार पर, रुपये के मूल्य पर सरकारी नियंत्रण कम करना।
- मुक्त व्यापार और निवेश नीतियाँ:
- अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने, विदेशी निवेश और प्रौद्योगिकी संलयन को बढ़ावा देने के लिए लक्षित।
- अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने, विदेशी निवेश और प्रौद्योगिकी संलयन को बढ़ावा देने के लिए लक्षित।
निजीकरण:
निजीकरण का अर्थ है उद्यमों के सरकारी स्वामित्व या प्रबंधन से निजी क्षेत्र के नियंत्रण में परिवर्तन।
निजीकरण के उद्देश्य:
- सरकार की वित्तीय स्थिति में सुधार करना।
- सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों पर कार्यभार कम करना।
- सरकारी संगठनों के व्यवस्थापन को बढ़ाना।
- उपभोक्ता को बेहतर माल और बेहतर सेवाएँ प्रदान करना।
- समाज में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का निर्माण करना।
- विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) को प्रोत्साहित करना।
विनीवेश और पूर्ण निजीकरण दो हथियार हैं। विनीवेश स्टॉक एक्सचेंजों पर शेयरों की बिक्री या रुचि रखने वाले खरीदारों को सीधे शेयर बेचकर प्राप्त किया जा सकता है। जबकि पूर्ण निजीकरण में सरकार निजी पक्षों को पूरी हिस्सेदारी या शेयर बेचती है।
भारत में विनीवेश प्रक्रिया: भारत में, वित्त मंत्रालय के तहत निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) विनीवेश प्रक्रिया की देखरेख करता है।
निजीकरण: कुछ सकारात्मक पहलू
- बढ़ी हुई दक्षता: निजी कंपनियां अधिक कुशल हो सकती हैं और बाजार बलों के प्रति तेजी से प्रतिक्रिया करने की संभावना रखती हैं, अंततः बेहतर सेवा वितरण के साथ लागत बचत प्रदान करती हैं।
- बढ़ा हुआ नवाचार: निजी प्रतिस्पर्धा नवाचार और तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देती है।
- सरकारी बोझ कम होना: निजीकरण राज्य के बोझ को कम करने में मदद करता है क्योंकि सरकार को कोई संसाधन वित्त पोषण की आवश्यकता नहीं होती है जिसका उपयोग अन्य विकास गतिविधियों में किया जा सकता है।
- विविधता में वृद्धि: उपभोक्ताओं के लिए अधिक विकल्प और विकल्प हैं जिनके पास निजी प्रदाताओं की अधिक उपलब्धता है।
निजीकरण के विरुद्ध तर्क:
- निजी बनाम सार्वजनिक हित: लाभ के लिए व्यवसाय, सार्वजनिक लक्ष्यों को पूरा करने के दबाव के बिना, सामाजिक कल्याण और सेवा की उपेक्षा कर सकते हैं। यह नौकरी छूटने का कारण बन सकता है क्योंकि निजी कंपनियां आमतौर पर दक्षता और लागत में कटौती के तरीकों पर ध्यान केंद्रित करती हैं, निजीकरण उन्हें व्यवसाय चलाने में बचाव दे सकता है।
- बाजार एकाधिकार: निजीकरण से एकाधिकारवादी बाजार बन सकते हैं जिसका अर्थ है कम प्रतिस्पर्धा और संभावित रूप से कीमतें बढ़ सकती हैं।
- पारदर्शिता का अभाव: निजी प्रक्रियाएं कम पारदर्शी हो सकती हैं क्योंकि अधिक गोपनीयता संभव है और ऐसे व्यवसाय हैं जहाँ सुधार हमेशा सार्वजनिक कल्याण की सेवा नहीं करते हैं, बल्कि व्यक्तिगत हितों को लाभान्वित करते हैं।
वैश्वीकरण:
वैश्वीकरण एक सतत आर्थिक सुधार है जो देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ता है। वैश्वीकरण को व्यापक रूप से वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एक राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के एकीकरण के रूप में माना जाता है, जिससे अधिक पारस्परिक निर्भरता और एकीकरण को बढ़ावा मिलता है।
वैश्वीकरण के उद्देश्य:
- आयात शुल्क कम करना
- विदेशी निवेशों को प्रोत्साहित करना
- विदेशी प्रौद्योगिकी में समझौते को प्रोत्साहन।
भारतीय अर्थव्यवस्था पर सुधारों का प्रभाव:
- उच्च विकास दर: 1990-91 में 5% से वर्ष 2007-08 के दौरान राष्ट्रीय आय बढ़कर 9.3% हो गई।
- राष्ट्रीय आय की संरचना में परिवर्तन: सुधार के बाद की अवधि में क्षेत्रों की संरचना नाटकीय रूप से बदल गई थी। जबकि कृषि का हिस्सा कम हुआ है, औद्योगिक और सेवा क्षेत्र में वृद्धि हुई है।
- बचत और निवेश: सुधार के बाद की अवधि में बचत और निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई।
- विदेशी व्यापार: निर्यात क्षेत्र धीरे-धीरे मुख्य विदेशी मुद्रा अर्जक में से एक बन गया है। उदाहरण के लिए, 2023 में भारत का कुल निर्यात (माल + सेवाएं) नवंबर 2023 तक 62.58 बिलियन अमरीकी डालर था।
- विदेशी मुद्रा भंडार: भुगतान संतुलन (BoP) में सुधार; सुधारों के बाद पुनरुत्थान हुआ। नतीजतन, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से बढ़ता है। 2022 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 647 बिलियन डॉलर है।
- विदेशी प्रत्यक्ष निवेश: भारत ने कुछ क्षेत्रों, जैसे लॉटरी व्यवसाय, चिट फंड, परमाणु ऊर्जा आदि को छोड़कर, अन्य क्षेत्रों में 100% एफडीआई का स्वागत किया। इसके अलावा, भारत ने भारतीय विनियमित पूंजी बाजार में निवेश करने के लिए विदेशी संस्थागत निवेशकों को अनुमति दी।
- मध्यम वर्ग का उदय: एमएनसी के आगमन और आपूर्ति-मांग गतिशीलता ने भारत की अर्थव्यवस्था में मध्यम वर्ग के उदय का कारण बना है।
नकारात्मक प्रभाव:
हालांकि भारत में एलपीजी सुधारों ने काफी नुकसान नियंत्रण किया, लेकिन उनके कुछ हानिकारक दुष्प्रभाव थे जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।
- मूल्य अस्थिरता: बाजार द्वारा निर्धारित मूल्य निर्धारण के लिए संक्रमण ने उपभोक्ताओं को अस्थिर कीमतों के प्रति कमजोर बना दिया।
- छोटे व्यवसायों पर प्रभाव: एलपीजी पर बहुत अधिक निर्भर व्यवसायों को अप्रत्याशित लागत का सामना करना पड़ा, जिससे उनकी लाभप्रदता और दीर्घकालिक व्यवहार्यता प्रभावित हुई।
- छोटे व्यवसायों पर प्रभाव: एलपीजी पर बहुत अधिक निर्भर व्यवसायों को अप्रत्याशित लागत का सामना करना पड़ा, जिससे उनकी लाभप्रदता और दीर्घकालिक व्यवहार्यता प्रभावित हुई।
- बाजार एकाग्रता: प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने का प्रारंभिक लक्ष्य पूरी तरह से महसूस नहीं हुआ, क्योंकि बाजार कुछ बड़े खिलाड़ियों, जैसे रिलायंस और एस्सार के आधिपत्य में आ गया।
- कम प्रतिस्पर्धा: एक ही कॉर्पोरेट इकाई के तहत क्षेत्रीय कंपनियों को एकीकृत करने के परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं को उत्पादों के वितरण और बिक्री को नियंत्रित करने वाली कम इकाइयां हुईं। हालांकि, कुछ खिलाड़ियों का दबदबा अभी भी उपभोक्ता विकल्प और इसलिए उनकी सौदेबाजी शक्ति को सीमित करता है।
- कम प्रतिस्पर्धा: एक ही कॉर्पोरेट इकाई के तहत क्षेत्रीय कंपनियों को एकीकृत करने के परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं को उत्पादों के वितरण और बिक्री को नियंत्रित करने वाली कम इकाइयां हुईं। हालांकि, कुछ खिलाड़ियों का दबदबा अभी भी उपभोक्ता विकल्प और इसलिए उनकी सौदेबाजी शक्ति को सीमित करता है।
- सुरक्षा संबंधी चिंताएँ:
- बढ़ी हुई दुर्घटनाएँ: एलपीजी वितरण नेटवर्क का तेजी से विस्तार और पारंपरिक आउटलेटों की बढ़ती संख्या ने सुरक्षा खतरों में वृद्धि की जिसके परिणामस्वरूप दुर्घटनाएं हुईं।
- नियमन और पर्यवेक्षण का अभाव: उदारीकरण पर प्रारंभिक ध्यान केंद्रित ने कम सख्त नियामक वातावरण का निर्माण किया, जिससे कुछ मामलों में दुर्घटनाओं और सुरक्षा खतरों में योगदान हुआ।
- बढ़ी हुई दुर्घटनाएँ: एलपीजी वितरण नेटवर्क का तेजी से विस्तार और पारंपरिक आउटलेटों की बढ़ती संख्या ने सुरक्षा खतरों में वृद्धि की जिसके परिणामस्वरूप दुर्घटनाएं हुईं।
- असमान विकास:
- क्षेत्रीय असमानताएँ: जबकि एलपीजी सुधारों से कुछ स्थानों को लाभ हुआ, वे पर्याप्त बुनियादी ढाँचे के समर्थन और वितरण नेटवर्क कनेक्टिविटी के साथ-साथ लगातार सीमित निवेश के कारण अन्य को प्राप्त करने में विफल रहे।
- सीमांत समुदायों का बहिष्कार: कुछ सीमांत समुदायों को अभी भी एलपीजी प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ा क्योंकि आर्थिक पृष्ठभूमि, भौगोलिक दूरस्थता और जागरूकता की कमी थी।
- क्षेत्रीय असमानताएँ: जबकि एलपीजी सुधारों से कुछ स्थानों को लाभ हुआ, वे पर्याप्त बुनियादी ढाँचे के समर्थन और वितरण नेटवर्क कनेक्टिविटी के साथ-साथ लगातार सीमित निवेश के कारण अन्य को प्राप्त करने में विफल रहे।
- पर्यावरण संबंधी चिंताएँ:
- रिसाव और उत्सर्जन: पारंपरिक ईंधन की तुलना में एक स्वच्छ ईंधन होने के बावजूद, उत्पादन, परिवहन और उपयोग चरणों में रिसाव और उत्सर्जन के संबंध में आशंका बनी हुई है जो हवा की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती है और जलवायु परिवर्तन का परिणाम हो सकती है।
- जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता: एलपीजी अभी भी एक जीवाश्म ईंधन है, और इस पर निरंतर निर्भरता में संभावित दीर्घकालिक आर्थिक व्यवहार्यता के साथ-साथ स्थिरता के मुद्दे भी हैं।
- रिसाव और उत्सर्जन: पारंपरिक ईंधन की तुलना में एक स्वच्छ ईंधन होने के बावजूद, उत्पादन, परिवहन और उपयोग चरणों में रिसाव और उत्सर्जन के संबंध में आशंका बनी हुई है जो हवा की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती है और जलवायु परिवर्तन का परिणाम हो सकती है।
आर्थिक सुधारों की आवश्यकता 2.0:
भारतीय अर्थव्यवस्था 2010 के दशक की शुरुआत से धीमी हो गई है, जिसमें COVID-19 महामारी के कारण मंदी और भी बदतर हो गई है। सीधे शब्दों में कहें तो, अर्थव्यवस्था को 2025 तक $5 ट्रिलियन GDP तक पहुँचने के लिए अपने स्पष्ट रूप से हानिकारक कानून की भरपाई करने के लिए और अधिक सुधार की आवश्यकता है।
लक्ष्य तक पहुँचने के लिए प्रमुख सुधार
- कर प्रणाली को सरल और सुव्यवस्थित करें: विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2022 के अनुसार, भारत को करों का भुगतान करने में आसानी में कुल 190 देशों में से 115वें स्थान पर रखा गया है।
- विनिर्माण को बढ़ावा दें: GDP में विनिर्माण के योगदान को तेज करने के लिए ठोस प्रयास, जो अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में बहुत कम है।
- विदेशी निवेश को बढ़ावा दें: भारत को आगामी सुधारों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है और विशेष रूप से अच्छे निवेश व्यवहार्यता की धारणा बनाने पर।
- उद्यमिता को बढ़ावा दें: स्टार्टअप और परिचालन के विस्तार के लिए बाधा कारकों को कम किया जाना चाहिए।
- कृषि उद्योग को बढ़ावा देना: भारत कृषि-समृद्ध है, लेकिन इसे मुश्किल से ही खरोंचा गया है।
- शिक्षा और कौशल के लिए संसाधन आवंटित करें: WEF के मानव पूंजी सूचकांक (HCindex) पर कुल नमूना देशों में से 116 के मानव पूंजी गुणवत्ता रेटिंग के साथ, भारत प्रतिस्पर्धी प्रक्रियाओं में आगे बढ़ने के लिए अपनी मानव संसाधन लाभांश का लाभ उठाने के लिए तैयार है।
- निर्यात को बढ़ावा दें: अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में एक प्रतियोगी के रूप में उभरने के लिए, भारत को अपने निर्यात प्रदर्शन में सुधार करने की आवश्यकता है।
2025 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था - क्या करें? परिचय: भारत सरकार ने देश में तेजी से आर्थिक विकास के लिए 2025 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा है। लक्ष्य को कैसे पूरा किया जाएगा:
- बुनियादी ढांचा विकास: बुनियादी ढाँचे में बड़े निवेश चल रहे हैं, मुख्य रूप से नौकरी सृजन और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के साथ-साथ उत्पादकता बढ़ाने के लिए।
- डिजिटल परिवर्तन: अधिकांश क्षेत्रों में, डिजिटलीकरण से नवाचार और अधिक दक्षता आ सकती है, जिससे नए प्रकार के व्यावसायिक अवसर पैदा होते हैं।
- कौशल कार्यक्रम: कौशल कार्यक्रमों का उद्देश्य कुशल कार्यबल में आगे बढ़ते हुए उद्योग की मांग को पूरा करना है, जबकि आर्थिक विकास को आगे बढ़ाना है।
- आईटी क्षेत्र का विस्तार: सिलिकॉन वैली के चैंपियन वे हैं जो 'वे बेचते हैं क्षमताएं', जो उद्यमियों को धन, सलाह और संसाधनों तक पहुँच प्रदान करके उनका समर्थन करता है जो नवाचार और व्यवसायों में सहायता करते हैं।
- सरलीकृत नियम प्रदान करें: लालफीताशाही को कम करें और भारतीय व्यवसायों को भारत में व्यापार करना आसान बनाएं।
सरकारी योजनाएँ:
भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर विकास और विकास के लिए या सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न आर्थिक कार्यक्रम शुरू किए हैं। कुछ लोकप्रिय कार्यक्रम हैं:
- मेक इन इंडिया: विनिर्माण और एफडीआई को बढ़ावा देने के लिए 2014 में घोषित किया गया।
- डिजिटल इंडिया: भारतीय समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए 2015 में लॉन्च किया गया।
- स्किल इंडिया: 2015 में योग्यता के लिए युवाओं के प्रशिक्षण और शिक्षा के उद्देश्य से लॉन्च किया गया।
- प्रधानमंत्री जन धन योजना: सभी के लिए बैंकिंग सुविधाएँ प्रदान करने और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए 2014 में लॉन्च किया गया।
हालांकि $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य आसान नहीं होगा, लेकिन भारत सरकार भारत में आर्थिक विकास और विकास को बढ़ावा देने के लिए कदम उठा रही है और उपाय शुरू कर रही है।
|
|
|

-1721391937657.png)