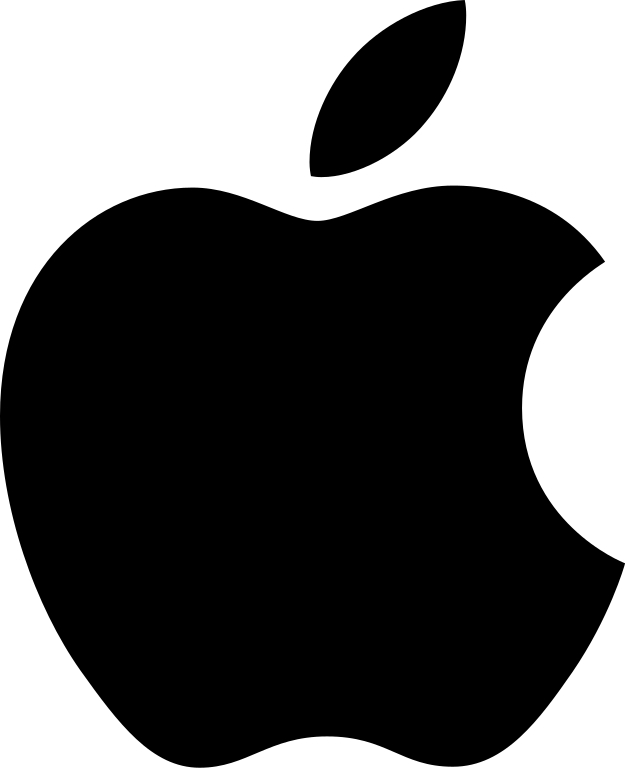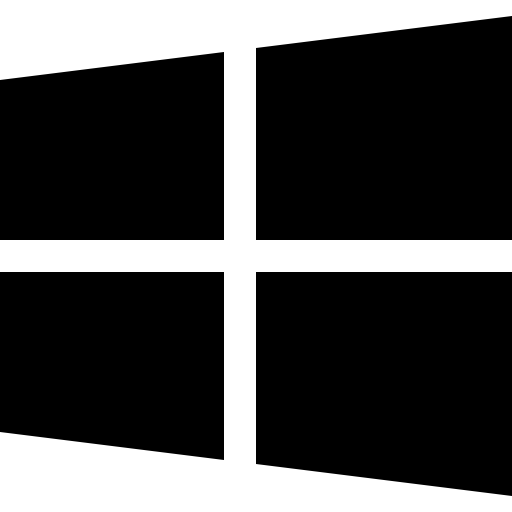न्यायिक पुनरावलोकन भारतीय लोकतांत्रिक ढांचे का एक प्रमुख तत्व है, जो यह सुनिश्चित करता है कि संविधान देश का सर्वोच्च कानून बना रहे। यह पोस्ट भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा, दायरा, महत्व और सीमाओं का विश्लेषण करती है।
न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ
न्यायिक पुनरावलोकन न्यायपालिका की वह शक्ति है जिसके तहत वह विधायी और कार्यकारी कार्रवाइयों की संवैधानिकता की जांच करती है। यदि कोई कानून या कार्य संविधान के विपरीत पाया जाता है, तो न्यायपालिका उसे शून्य और अमान्य घोषित कर सकती है।
संवैधानिक प्रावधान
-
अनुच्छेद 13:
- मौलिक अधिकारों के विपरीत कानूनों को शून्य घोषित करता है।
- न्यायपालिका को संविधान पूर्व और संविधान पश्चात कानूनों की समीक्षा का अधिकार देता है।
-
अनुच्छेद 32 और 226:
- मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को उपाय प्रदान करते हैं।
-
अनुच्छेद 131, 132, 133 और 134:
- सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार को परिभाषित करते हैं, जिससे न्यायिक पुनरावलोकन सक्षम होता है।
-
अनुच्छेद 136:
- सर्वोच्च न्यायालय को विशेष अनुमति याचिका के माध्यम से अपील स्वीकार करने का अधिकार देता है।
-
अनुच्छेद 143:
- संविधान से जुड़े मामलों में सर्वोच्च न्यायालय को परामर्शी अधिकार देता है।
न्यायिक पुनरावलोकन का दायरा
भारत में न्यायिक पुनरावलोकन निम्नलिखित क्षेत्रों को कवर करता है:
-
विधायी कार्रवाइयां:
- न्यायपालिका यह सुनिश्चित करती है कि विधायिका द्वारा पारित कानून संविधान के अनुरूप हों।
-
कार्यकारी कार्रवाइयां:
- प्रशासनिक निर्णयों और सरकारी आदेशों की समीक्षा शामिल है।
-
संवैधानिक संशोधन:
- "मूल संरचना सिद्धांत" के तहत संविधान संशोधन भी न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत आते हैं, जैसा कि केशवानंद भारती केस (1973) में स्थापित किया गया।
महत्व
-
संवैधानिक सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है:
- यह सुनिश्चित करता है कि सभी कानून और कार्रवाइयां संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप हों।
-
मौलिक अधिकारों की रक्षा:
- विधायिका और कार्यपालिका की मनमानी कार्रवाईयों से रक्षा करता है।
-
संघीय संतुलन बनाए रखता है:
- केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को हल करता है।
-
जवाबदेही बढ़ाता है:
- सार्वजनिक प्राधिकरणों के शक्ति दुरुपयोग पर रोक लगाता है।
सीमाएं
-
शक्ति पृथक्करण सिद्धांत:
- न्यायपालिका को विधायिका और कार्यपालिका की स्वायत्तता का सम्मान करना चाहिए।
-
संसदीय संप्रभुता:
- संसद न्यायिक व्याख्याओं को निष्प्रभावी करने के लिए कानूनों में संशोधन कर सकती है।
-
न्यायिक अतिरेक:
- आलोचकों का तर्क है कि अत्यधिक न्यायिक हस्तक्षेप शासन को बाधित कर सकता है।
-
केवल संवैधानिक अनुपालन तक सीमित:
- न्यायिक पुनरावलोकन नीतिगत निर्णयों की योग्यता का आकलन नहीं करता।
प्रमुख मामले
-
ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य (1950):
- मौलिक अधिकारों और न्यायिक पुनरावलोकन पर पहला प्रमुख मामला।
-
केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973):
- मूल संरचना सिद्धांत स्थापित किया गया।
-
मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978):
- मौलिक अधिकारों का दायरा बढ़ाया।
-
मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ (1980):
- मूल संरचना सिद्धांत को मजबूत किया।
निष्कर्ष
न्यायिक पुनरावलोकन लोकतंत्र, कानून के शासन और व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं को बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण तंत्र है। हालांकि इसकी सीमाएं हैं, यह यह सुनिश्चित करता है कि सभी शक्तियों का प्रयोग संवैधानिक दायरे में हो।

-1721391937657.png)