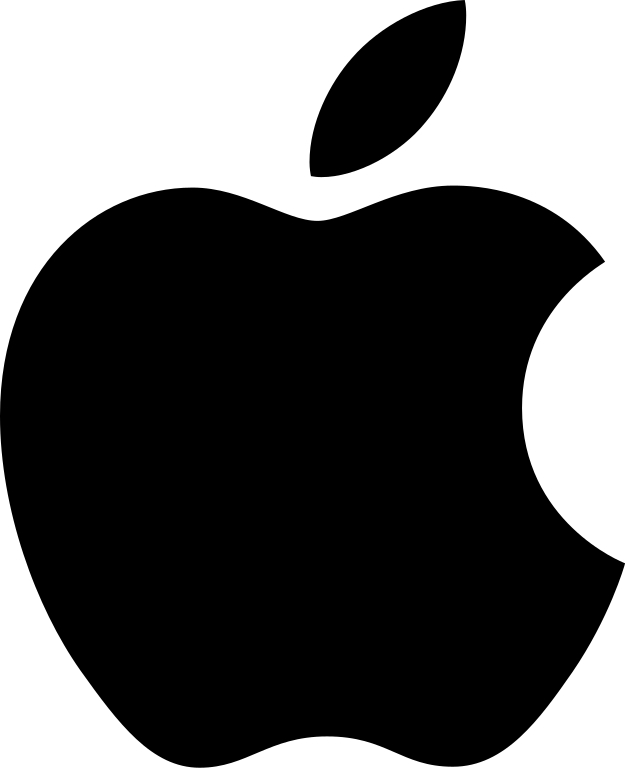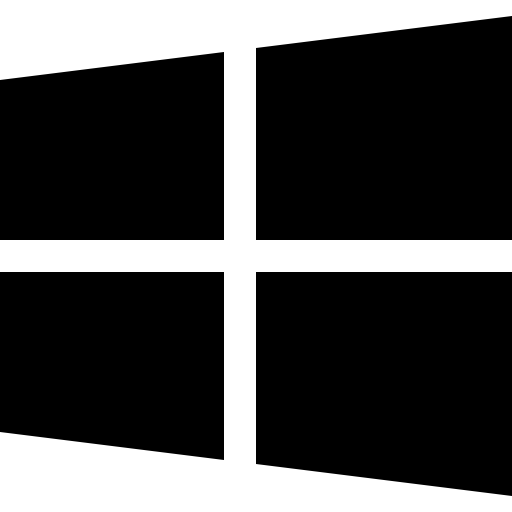सविनय अवज्ञा आंदोलन (1930-1934), जिसे महात्मा गांधी ने नेतृत्व किया, भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई का एक महत्वपूर्ण चरण था। यह ऐतिहासिक Salt March से शुरू हुआ, जो 12 मार्च 1930 को हुआ, जब गांधी और उनके अनुयायियों ने ब्रिटिश नमक कर का विरोध करते हुए दांडी के लिए 240 मील की दूरी तय की। इस अहिंसक प्रतिरोध ने लाखों भारतीयों को औपनिवेशिक कानूनों को तोड़ने के लिए प्रेरित किया, जिससे बड़े पैमाने पर विरोध, बहिष्कार और करों का भुगतान न करने की घटनाएं हुईं। इस आंदोलन का लक्ष्य स्वराज (स्व-शासन) प्राप्त करना था और इसने ब्रिटिश शासन पर दबाव बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन इससे पहले के प्रयासों की तुलना में अधिक आक्रामक तरीके से।
सिविल नाफरमानी आंदोलन का उद्देश्य और रणनीति Non-Cooperation Movement (1920-1922) से भिन्न था। जबकि दोनों ने अहिंसक प्रतिरोध को बढ़ावा दिया, गैर-ग cooperación आंदोलन ने भारतीयों से ब्रिटिश संस्थानों, जैसे स्कूलों और अदालतों, से दूर रहने का आग्रह किया। इसके विपरीत, सिविल नाफरमानी आंदोलन ने अन्यायपूर्ण कानूनों और नीतियों को सीधे चुनौती देकर एक कदम आगे बढ़ाया, जिसका उद्देश्य न केवल भारतीयों को ब्रिटिश शासन से दूर करना था, बल्कि जानबूझकर नाफरमानी के कार्यों के माध्यम से इसे चुनौती देना भी था।
हमारा UPSC तैयारी कोर्स, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों उपलब्ध है, भारतीय और विश्व इतिहास का व्यापक अध्ययन प्रदान करता है। MalukaIAS Courses में महत्वपूर्ण वैश्विक घटनाओं, जैसे पुनर्जागरण, औद्योगिक क्रांति, और विश्व युद्धों पर चर्चा की जाती है, और उनके आधुनिक समाज पर प्रभाव को उजागर किया जाता है। हमारा GS फाउंडेशन एडवांस बैच 2025 भी UPSC पाठ्यक्रम के साथ अच्छी तरह से संरचित मॉड्यूल प्रदान करता है, जिससे छात्रों को सभी विषयों और उनकी प्रासंगिकता का गहरा ज्ञान प्राप्त होगा। चाहे आप हमारे इतिहास-ऑप्शनल 2025 कोर्स (ऑनलाइन और ऑफलाइन) या test series का विकल्प चुनें, यह कार्यक्रम उम्मीदवारों को UPSC परीक्षाओं के इतिहास खंड में महारत हासिल करने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
सविनय अवज्ञा आंदोलन की पृष्ठभूमि
असहयोग आंदोलन के परिणाम:
Non-Cooperation Movement (1920-22) (असहयोग आंदोलन) चौरी चौरा घटना के बाद अचानक समाप्त कर दिया गया, लेकिन इससे जनतांत्रिक चेतना जाग उठी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) ब्रिटिश सरकार की कठोरता के जवाब में पूर्ण स्वराज (पूर्ण स्वतंत्रता) की मांग करती रही।
साइमन कमीशन (1927):
ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त साइमन कमीशन, जो भारत में संवैधानिक सुधारों का सुझाव देने के लिए बनाया गया था, जिसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, के कारण व्यापक प्रदर्शन हुए। कमीशन की रिपोर्ट, जिसे बाद में सिफारिशों के रूप में जाना गया, ने भारतीयों में आत्म-प्रशासन की मांग को और बढ़ावा दिया।
पूर्ण स्वराज (स्वतंत्रता की घोषणा) (1929):
दिसंबर 1929 में लाहौर सत्र में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में पूर्ण स्वतंत्रता (पूर्ण स्वराज) को लक्ष्य घोषित किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 26 जनवरी, 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में घोषित किया गया और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का संकल्प लिया गया।
वैश्विक आंदोलनों का प्रभाव:
दुनिया भर में अहिंसक प्रतिरोध की सफलताओं (जैसे अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन या आयरलैंड में ब्रिटिश शासन के खिलाफ) ने गांधी और भारतीय आंदोलन को व्यापक रूप से सूचित किया।
सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण
आर्थिक शोषण:
ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियां, जैसे भारी कराधान, भारतीय संसाधनों का दोहन, और प्रतिकूल व्यापारिक प्रथाओं ने भारत की कृषि और उद्योग को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। भारतीय जनता की खराब होती आर्थिक स्थिति ने उनके दबे हुए क्रोध को विद्रोही मूड में बदलने का अतिरिक्त दबाव डाला।
नमक कर:
ब्रिटिशों ने नमक कर भी लगाया, जिससे भारतीयों को अपना नमक बनाने या बेचने से रोका गया और इससे गरीबों को सबसे अधिक नुकसान हुआ। यह, गांधी के अनुसार, ब्रिटिश उत्पीड़न का प्रतीक था और इसीलिए उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया।
दमनकारी कानून:
रॉलेट एक्ट (1919) जैसे दमनकारी कानूनों ने ब्रिटिशों को बिना मुकदमे के भारतीयों को गिरफ्तार करने की अनुमति दी, जिससे असंतोष अत्यधिक बढ़ गया। औपनिवेशिक उत्पीड़न के रूप में देखे जाने वाले इन कानूनों ने आत्म-शासन की मांग को बढ़ाया।
अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ:
भारत में यह असंतोष महान मंदी (1929) के प्रभाव से बढ़ गया, जिसने उनकी पहले से ही खराब होती अर्थव्यवस्था को और बिगाड़ दिया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद के विकास ने औपनिवेशिक साम्राज्यों में आत्म-निर्णय आंदोलनों की दिशा में वैश्विक बदलाव किया, जिससे भारतीय नेताओं ने स्वतंत्रता की ओर ज्यादा दबाव डाला।
सुधार:
ब्रिटिश ने कई बार संवैधानिक सुधारों का प्रयास किया। मोंटेग्यू-शेम्सफ़र्ड सुधार, भारत सरकार अधिनियम 1919, जो अपर्याप्त थे और प्रमुख दलों की अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर सके. ऊपरी स्तर पर औपचारिक आत्म-शासन मिला। चूंकि ये सुधार भारतीयों की पूरी स्वतंत्रता की अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर सके, एक नए मिक्स मंत्र की पेशकश की गई जो अधिक प्रत्यक्ष कार्रवाई की मांग करता था।
सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रतिक्रियाएँ
1. वैश्विक ध्यानाकर्षण: यह आंदोलन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुख्यात हो गया और वैश्विक समर्थन प्राप्त किया, जिससे ब्रिटिश सरकार पर भारी दबाव पड़ा।
2. एकता और सशक्तिकरण: इसने विभिन्न धर्मों, जातियों और क्षेत्रों के भारतीयों को एक साथ लाया, जिससे एक सामूहिक राष्ट्रीय पहचान की नींव पड़ी।
3. अहिंसात्मक प्रतिरोध: इसने अहिंसात्मक प्रतिरोध की प्रभावशीलता का प्रदर्शन किया, जिससे दुनिया भर में अन्य समान आंदोलनों को प्रेरणा मिली।
4. राजनीतिक सफलता: यह आंदोलन ब्रिटिशों से व्यापक स्वायत्तता प्राप्त करने में सफल रहा, पहले डोमिनियन का दर्जा और फिर स्वतंत्रता मिली।
5. धार्मिक सुधार: इसने भारत में धार्मिक सुधारों को उत्प्रेरित किया, विशेष रूप से अस्पृश्यता और लैंगिक समानता के संदर्भ में।
6. हिंसा और दमन: हालांकि आंदोलन पूरी तरह से अहिंसात्मक था, ब्रिटिश अधिकारियों ने इस पर व्यापक हिंसा और दमन किया, जिसके परिणामस्वरूप सैकड़ों से लेकर हजारों लोगों की मृत्यु हुई।
7. आर्थिक मंदी: ब्रिटिश उद्योगों पर निर्भर विपुल भारतीयों की आजीविका, बहिष्कार और हड़तालों से प्रभावित हुई।
8. विभाजन और संघर्ष: आंदोलन ने कार्रवाई के मुद्दों का सामना किया, विशेष रूप से संभावित रणनीति और लक्ष्यों के संबंध में, जिससे आंतरिक संघर्ष और प्रतिद्वंद्विता उत्पन्न हुई।
9. सीमित प्रभाव: हालांकि आंदोलन ने सामान्य रूप से स्वतंत्रता प्राप्त की, इसका कुछ हाशिए के समूहों जैसे महिलाओं और निचली जातियों पर प्रभाव मामूली था।
सविनय अवज्ञा आंदोलन की कमियाँ (Drawbacks)
1. परिभाषित रणनीति की कमी: कभी-कभी आंदोलन में सामंजस्य की कमी दिखी, रणनीति में महत्वपूर्ण विविधताएं और अस्पष्टताएं थीं।
2. गांधीवादी नेतृत्व पर निर्भरता: आंदोलन की भारी निर्भरता - और गांधी स्वयं - बार-बार प्रश्नचिन्ह बन गई, जिससे उनकी अनुपस्थिति या सीमितता में अहिंसात्मक पद्धति खतरे में पड़ गई।
3. संकीर्ण सामाजिक आधार: आंदोलन ने ग्रामीण भारत जैसे कुछ क्षेत्रों में केवल सीमित सामाजिक आधार प्राप्त किया; इसका प्रभाव सार्वजनिक क्षेत्रों में विशेष रूप से कम था।
4. राजनीति पर दीर्घकालिक प्रभाव: अहिंसा पर जोर, हालांकि औपनिवेशिक साम्राज्यवाद से छुटकारा पाने में सफल रहा, लेकिन मजबूत राजनीतिक संस्थानों और एक कार्यशील नागरिक समाज को विकसित करने की क्षमता को प्रभावित किया।
सविनय अवज्ञा आंदोलन का महत्व (Significance)
1. अहिंसात्मक विरोध: आंदोलन ने अहिंसा (अहिंसा) के सिद्धांत पर आधारित था। प्रतिभागियों ने ब्रिटिश सरकार के कुछ कानूनों, मांगों और आदेशों का शांतिपूर्वक पालन करने से इनकार किया।
2. नमक मार्च: इस आंदोलन की सबसे प्रतीकात्मक घटनाओं में से एक थी नमक मार्च (डांडी मार्च) 1930 में। गांधी ने अपने अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से डांडी तक मार्च किया और समुद्र के पानी से नमक बनाया, ब्रिटिश नमक उत्पादन पर एकाधिकार को ठुकराते हुए।
3. विविध भागीदारी: आंदोलन ने भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों से व्यापक भागीदारी देखी जिसमें पुरुष, महिलाएं, युवा और वृद्ध शामिल थे, जो विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक पृष्ठभूमि से थे।
4. व्यापक पैमाना: यह सिर्फ शहरी क्षेत्रों तक सीमित नहीं था; ग्रामीण क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण भागीदारी देखी गई। इसमें ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार, करों का भुगतान न करना और सरकारी नौकरियों से इस्तीफा देना शामिल था।
5. अंतर्राष्ट्रीय ध्यान: इसने भारतीयों की ब्रिटिश शासन के तहत दुर्दशा पर महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया और अहिंसात्मक प्रतिरोध की प्रभावशीलता को उजागर किया।
6. ब्रिटिश प्रतिक्रिया: ब्रिटिश सरकार ने शुरू में दमन के माध्यम से प्रतिक्रिया दी, हजारों कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया, जिसमें गांधी भी शामिल थे। हालांकि, इसने भारतीय लोगों के संकल्प को और बढ़ाया और वैश्विक सहानुभूति अर्जित की।
7. स्वतंत्रता संघर्ष पर प्रभाव: सविनय अवज्ञा आंदोलन ने औपनिवेशिक शासन के खिलाफ भारतीय समाज को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, एकता और राष्ट्रीय चेतना का निर्माण किया। इसने भविष्य के आंदोलनों के लिए नींव रखी और अंततः 1947 में भारत को स्वतंत्रता दिलाने में योगदान दिया।
सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रसार
गुजरात
- नमक मार्च और डांडी: महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम से डांडी तक के नमक मार्च ने एक महत्वपूर्ण घटना को जन्म दिया। हजारों लोगों ने नमक कर के विरोध में गांधी का अनुसरण किया। इस कृत्य ने राज्य के अन्य हिस्सों में समान विरोधों को प्रेरित किया।
- आर्थिक बहिष्कार: लोगों ने ब्रिटिश वस्त्रों का बहिष्कार किया, विशेष रूप से विदेशी कपड़े का, और खादी के उपयोग को बढ़ावा दिया।
तमिलनाडु
- वेदारन्यम मार्च: सी. राजगोपालाचारी ने त्रिचिनापल्ली से वेदारन्यम तक एक नमक मार्च का नेतृत्व किया, यह गांधी के डांडी मार्च जैसा ही था। मार्च में शामिल लोगों ने समुद्र से नमक इकट्ठा किया, जो ब्रिटिश कानूनों का उल्लंघन था।
- छात्र भागीदारी: मद्रास (अब चेन्नई) के छात्र ब्रिटिश नियंत्रित शैक्षणिक संस्थानों का सक्रिय रूप से बहिष्कार कर रहे थे।
बंगाल
- प्रदर्शन और बहिष्कार: बंगाल में, सविनय अवज्ञा में कर न चुकाना, ब्रिटिश वस्त्रों का बहिष्कार और शराब की दुकानों पर धरना देना शामिल था।
- सांस्कृतिक जुटाव: बंगाल में आंदोलन सांस्कृतिक और बौद्धिक जुटाव द्वारा चिह्नित था, जिसमें लेखकों और कवियों ने राष्ट्रीयता के कारण को बढ़ावा दिया।
महाराष्ट्र
- कोई कर अभियान नहीं: महाराष्ट्र के किसानों ने भूमि राजस्व और अन्य करों का भुगतान करने से इनकार कर दिया, जिससे ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा व्यापक जमीन और संपत्ति की जब्ती हुई।
- शहरी गतिविधियाँ: मुंबई जैसे शहरों में बड़े पैमाने पर ब्रिटिश वस्त्रों और संस्थानों का बहिष्कार हुआ।
पंजाब
- प्रदर्शन और हड़तालें: बड़े पैमाने पर प्रदर्शन और हड़तालें आम थीं, जिनमें लाला लाजपत राय जैसे नेता लोगों को आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित करते थे।
- किसान विद्रोह: ग्रामीण पंजाब में किसानों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, करों का भुगतान करने से इनकार किया और ब्रिटिश अधिकारियों को चुनौती दी।
उत्तर प्रदेश
- कर ना चुकाने का विरोध: बलिया और गोरखपुर जैसे क्षेत्रों में, लोगों ने कर नहीं चुकाए, जिससे ब्रिटिश द्वारा संपत्ति की जब्ती और कड़ी सजा हुई।
- युवाओं की भूमिका: इलाहाबाद और वाराणसी जैसे स्थानों में छात्रों और युवा नेताओं ने आंदोलन के प्रसार में सक्रिय भाग लिया।
बिहार
- किसानों का जुटाव: राजेंद्र प्रसाद जैसे प्रभावशाली नेताओं ने किसानों को कर और राजस्व का भुगतान न करने के लिए जुटाया, जिसके परिणामस्वरूप ब्रिटिश अधिकारियों से महत्वपूर्ण संघर्ष हुए।
- शहरी केंद्र: पटना जैसे शहरों में ब्रिटिश वस्त्रों और संस्थानों का सक्रिय बहिष्कार देखा गया।
कर्नाटक
- नमक सत्याग्रह: कर्नाटक में नमक सत्याग्रह ने गति पकड़ी और लोगों ने तटीय क्षेत्रों में नमक कानूनों की अवहेलना की।
- स्थानीय नेतृत्व: निट्टूर श्रीनिवास राव जैसे नेताओं ने प्रदर्शनों को संगठित करने और राज्य भर में आंदोलन फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
आंध्र प्रदेश
- चौधरी बंधु: मद्रास प्रेसिडेंसी में, जिसमें आधुनिक आंध्र प्रदेश के हिस्से शामिल थे, चौधरी बंधु जैसे नेताओं ने ब्रिटिश कानूनों के खिलाफ विरोध संगठित किए।
- सविनय अवज्ञा: तटीय क्षेत्रों के लोगों ने नमक सत्याग्रह में भाग लिया और ब्रिटिश वस्त्रों का बहिष्कार किया।
केरल
- वैकोम सत्याग्रह: हालांकि यह सविनय अवज्ञा आंदोलन से पहले की घटना थी, लेकिन वैकोम सत्याग्रह ने प्रेरणा दी। सविनय अवज्ञा के युग में, केरल में लोगों ने नमक विरोध और बहिष्कार में सक्रिय भाग लिया।
- आर्थिक बहिष्कार: निवासियों ने विदेशी कपड़े और शराब की दुकानों का प्रमुखता से बहिष्कार किया।
असम
- चाय बागान: चाय बागानों के श्रमिकों ने आंदोलन में भाग लिया, ब्रिटिश द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को अस्वीकार किया और बहिष्कार में भाग लिया।
- शैक्षिक विरोध: शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों की महत्वपूर्ण भागीदारी देखी गई।
ओडिशा (उड़ीसा)
- नमक मार्च: गांधी से प्रेरित होकर, स्थानीय नेताओं ने ओडिशा में नमक मार्च का आयोजन किया और ब्रिटिश नमक कानूनों को चुनौती दी।
- आर्थिक बहिष्कार: ब्रिटिश वस्त्रों और सेवाओं का बहिष्कार एक व्यापक गतिविधि थी।
राजस्थान
- किसान आंदोलनों: राजस्थान के किसानों के आंदोलन, विशेष रूप से रियासती राज्यों में, सविनय अवज्ञा आंदोलन के अभिन्न अंग बन गए।
- शहरी प्रदर्शन: जयपुर जैसे शहरी केंद्रों में महत्वपूर्ण राजनीतिक सक्रियता और आर्थिक बहिष्कार में भागीदारी देखी गई।
सिंध और उत्तर-पश्चिम सीमा प्रांत
- नमक सत्याग्रह: आधुनिक पाकिस्तान के क्षेत्रों जैसे सिंध और उत्तर-पश्चिम सीमा प्रांत में नमक सत्याग्रह और प्रदर्शन में सक्रिय भागीदारी देखी गई।
- खान अब्दुल गफ्फार खान: उत्तर-पश्चिम सीमा प्रांत में, खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसने गांधी के अहिंसा और सविनय अवज्ञा के सिद्धांतों के साथ निकटता से संरेखित किया।
मध्य प्रांत और बरार
- कर ना चुकाना: कृषि क्षेत्रों में गाँव के निवासियों ने कर और राजस्व का भुगतान करने से इनकार कर दिया।
- शैक्षिक बहिष्कार: क्षेत्र भर में छात्रों ने ब्रिटिश शैक्षणिक संस्थानों का सक्रिय बहिष्कार किया।
कश्मीर
- राजनीतिक जुटाव: यद्यपि रियासती शासन के अधीन और कुछ हद तक अलग-थलग, कश्मीर ने राजनीतिक चेतना में वृद्धि देखी, जिससे बड़े आंदोलन को नैतिक और आर्थिक समर्थन मिला।

-1721391937657.png)