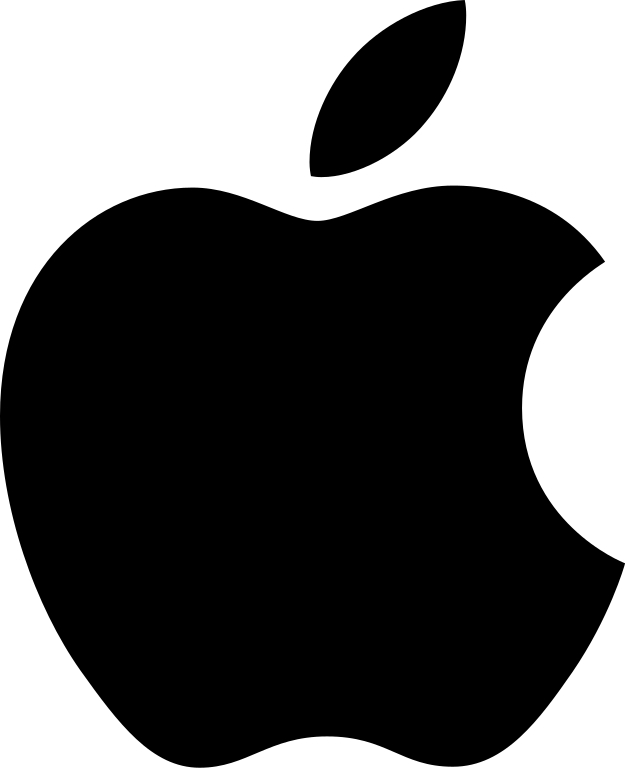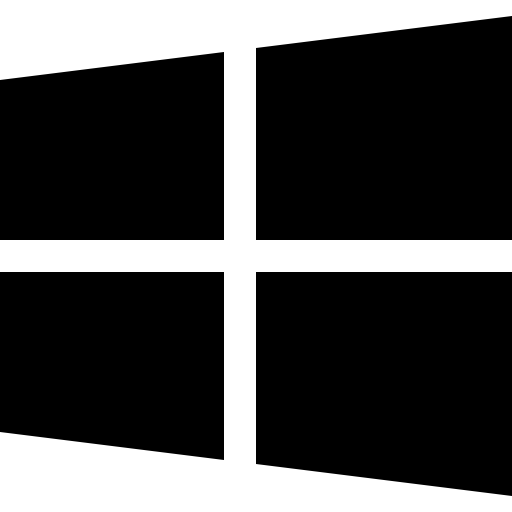आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में संशोधन करने वाले हालिया विधेयक का उद्देश्य आपदा प्रतिक्रिया दक्षता को बढ़ाना और एनडीएमए की भूमिका का विस्तार करना है, लेकिन इसकी संस्थागत स्थिति को मजबूत करने की उपेक्षा की गई है।
क्या आप जानते हैं?
IAS उम्मीदवारों के लिए आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक 2024 जैसे विधायी परिवर्तनों के साथ अपडेट रहना अत्यंत महत्वपूर्ण है। मालुका IAS अकादमी के to the point Current Affairs notes आपको ऐसे महत्वपूर्ण विषयों के बारे में अद्यतन रखने में मदद करते हैं, जिससे आपकी परीक्षा की तैयारी और प्रभावी हो जाती है।
जैसे आपदा प्रबंधन रणनीतियों में सुधार आवश्यक होता है, वैसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं को पास करने के लिए एक अच्छी तैयारी योजना की आवश्यकता होती है। मालुका IAS अकादमी का GS Foundation Advance Batch 2025 आपको सफलता के लिए आवश्यक नींव प्रदान करता है।
संशोधन और आपदा संबंधित नीतियों का विश्लेषण निरंतर अभ्यास की मांग करता है, जैसे कि परीक्षाओं की तैयारी। मालुका IAS अकादमी के Prelims and Mains Test Series, छात्र अपनी कौशल को निखार सकते हैं और IAS और PCS परीक्षाओं की चुनौतियों का आत्मविश्वास के साथ सामना कर सकते हैं।
IAS उम्मीदवारों के लिए आपदा प्रबंधन विधेयक जैसे प्रमुख विषयों के बारे में अद्यतन रहना महत्वपूर्ण है। Maluka IAS Academy का GS फाउंडेशन बैच इन विषयों को व्यापक रूप से कवर करता है ताकि आप परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकें।
जैसे आपदाएँ किसी देश की सहनशीलता की परीक्षा लेती हैं, वैसे ही प्रतियोगी परीक्षाएँ उम्मीदवारों की तैयारी और संकल्प की परीक्षा लेती हैं। मालुका IAS अकादमी का Punjab PCS Online कोचिंग आपको इन चुनौतियों को पार करने और सफलता प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है।
आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005
आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 भारत में आपदा प्रबंधन के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करता है, जिसमें प्रभावी प्रबंधन, जोखिम न्यूनीकरण और पुनर्वास पर 11 अध्याय और 79 धाराएं शामिल हैं।
आपदा प्रबंधन अधिनियम का उद्देश्य
- नीतियाँ: आपदा प्रबंधन नीतियों का निर्माण और कार्यान्वयन
- आपदा रोकथाम और न्यूनीकरण: आपदा की रोकथाम और न्यूनीकरण के लिए तैयारी और क्षमता निर्माण को बढ़ाता है
- आपदा राहत: प्रभावित राज्यों और व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है
डीएम अधिनियम 2005 का कानूनी-संस्थागत ढांचा
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत वित्तपोषण संरचना
आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 दो प्रमुख साधनों के साथ वित्तपोषण ढांचा प्रदान करता है:
- राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF): केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित, यह एनडीएमए नियमों द्वारा निर्देशित, आपदाओं के दौरान तत्काल राहत और पुनर्वास का समर्थन करता है।
- राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF): स्थानीय आपदा जरूरतों को पूरा करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के योगदान के साथ, एनडीआरएफ द्वारा पूरक राज्य स्तरीय कोष
आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 का महत्व
- संस्थागत ढांचा: अधिनियम ने आपदा अनुसंधान, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए एनडीएमए, एसडीएमए, एनडीआरएफ और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (NIDM) की स्थापना की।
- आपदा न्यूनीकरण: इस ढांचे ने प्रभावी रूप से लोगों की जान बचाई है तथा राहत, बचाव और पुनर्वास प्रदान किया है।
- जोखिम न्यूनीकरण: अधिनियम आपदा प्रबंधन को विकास योजना में एकीकृत करता है, जैसा कि 2009 की राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति और 2016 की राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना में देखा गया है।
- संसाधन आवंटन: आपदा प्रतिक्रिया और राहत में समय पर वित्तीय सहायता के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की स्थापना की जाती है।
- सामुदायिक भागीदारी: आपदा प्रबंधन में स्थानीय प्राधिकारियों और सामुदायिक समूहों की भूमिका पर जोर दिया जाता है।
भारत में आपदा प्रबंधन अधिनियम की चुनौतियाँ
संस्थागत चुनौतियाँ
- रिक्त उपाध्यक्ष पद: एक दशक से चली आ रही रिक्ति के कारण नेतृत्व और राजनीतिक प्रभाव की कमी
- सीमित वित्तीय शक्तियाँ: गृह मंत्रालय के माध्यम से निर्णय लेने में अक्षमता
- कर्मचारियों की कमी: छह या सात से नीचे केवल तीन सदस्य, परिचालन क्षमता को प्रभावित कर रहे हैं
- संकट में अदृश्यता: खराब परियोजना योजना और निष्पादन के लिए आलोचना की गई, विशेष रूप से COVID-19 जैसी प्रमुख घटनाओं के दौरान
कार्यात्मक चुनौतियाँ
- डीआरआर प्रयासों की प्राथमिकता और एकीकरण में अप्रभावीता: डीआरआर में विकासात्मक गतिविधियों के साथ एकीकरण का अभाव है।
- सार्वजनिक स्वास्थ्य संकटों का अप्रभावी निवारण: महामारी और जैव आतंकवाद के लिए अपर्याप्त प्रावधान।
- मानव निर्मित खतरों और जलवायु परिवर्तन पर सीमित जोर: प्रणालीगत जलवायु और मानव निर्मित आपदाओं पर अपर्याप्त ध्यान।
- केंद्रीकृत दृष्टिकोण: ऊपर से नीचे की कार्यप्रणाली स्थानीय और समुदाय-आधारित हस्तक्षेपों की उपेक्षा करती है।
वित्तपोषण की चुनौतियाँ
- अपर्याप्त फंडिंग: बड़े पैमाने पर आपदाओं के दौरान अपर्याप्त फंड प्रतिक्रिया और पुनर्प्राप्ति प्रयासों में देरी करते हैं
- नौकरशाही देरी: धन संवितरण में नौकरशाही बाधाएँ समय पर सहायता में बाधा डालती हैं
आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक 2024 में प्रमुख संशोधन
- शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण: समन्वित शहरी आपदा प्रतिक्रिया के लिए प्रमुख शहरों में नगर निगम आयुक्तों की अध्यक्षता में प्राधिकरणों की स्थापना की जाती है।
- राज्यों के लिए अनिवार्य एसडीआरएफ: सभी राज्यों को वर्तमान विसंगतियों को दूर करते हुए एक राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) की स्थापना और रखरखाव करना आवश्यक है।
- एनसीएमसी को कानूनी दर्जा: प्रमुख राष्ट्रीय आपदाओं के लिए नोडल निकाय के रूप में राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति (एनसीएमसी) को कानूनी दर्जा प्रदान किया गया है।
- एनडीएमए की बढ़ी हुई भूमिका: उभरते खतरों सहित आपदा जोखिमों की एक व्यापक श्रेणी को कवर करने के लिए एनडीएमए की जिम्मेदारियों का विस्तार किया गया है।
- आपदा योजना तैयार करना: आपदा योजना तैयार करने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय और राज्य कार्यकारी समितियों से हटाकर एनडीएमए और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों को सौंप दी गई है।
- आपदा डेटाबेस: एनडीएमए और एसडीएमए को क्रमशः राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय आपदा डेटाबेस बनाने और बनाए रखने का अधिकार दिया गया है।
- मुआवजा संबंधी दिशानिर्देश: एनडीएमए आपदा प्रभावित व्यक्तियों के लिए न्यूनतम राहत मानकों और मुआवजे की सिफारिश करेगा।
- आपदा परिभाषा स्पष्टीकरण: कानून-व्यवस्था संबंधी मुद्दों, जैसे दंगे, के कारण होने वाली मानव-निर्मित आपदाओं को आपदा परिभाषा से बाहर रखा गया है।
आगे की राह
- परिभाषाओं में संशोधन: सुसंगतता के लिए 'खतरों', 'रोकथाम' और 'शमन' की स्पष्ट परिभाषाएं शामिल करने के लिए धारा 2 में संशोधन करना।
- आपदा निवारण अध्याय: व्यापक आपदा निवारण योजनाओं पर ध्यान केन्द्रित करने वाले अध्याय प्रस्तुत करना।
- जवाबदेही में वृद्धि: आधिकारिक जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए न्यायिक निगरानी को बढ़ाना।
- आधुनिकीकृत पूर्व चेतावनी प्रणालियाँ: बेहतर पूर्वानुमान और प्रतिक्रिया के लिए जीआईएस और एआई जैसी प्रौद्योगिकियों को एकीकृत करने के लिए पूर्व चेतावनी प्रावधानों को अद्यतन करना।
- समुदाय और नीति निर्माता सहभागिता: सामुदायिक जागरूकता को बढ़ावा दें तथा आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन प्रयासों में नीति निर्माताओं को शामिल करें।
- विशेष संसाधन आवंटन: पर्याप्त वित्तपोषण सुनिश्चित करने के लिए आपदा प्रबंधन के लिए विशिष्ट वार्षिक बजट आवंटित करना।
इन सिफारिशों के कार्यान्वयन से आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की प्रभावशीलता बढ़ेगी तथा आपदा प्रबंधन के प्रति सक्रिय एवं संगठित दृष्टिकोण को बढ़ावा मिलेगा।

-1721391937657.png)