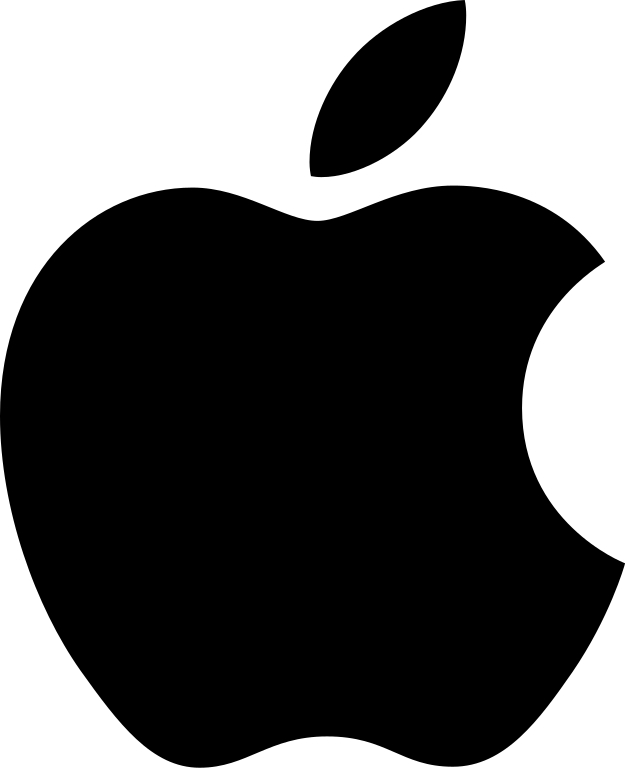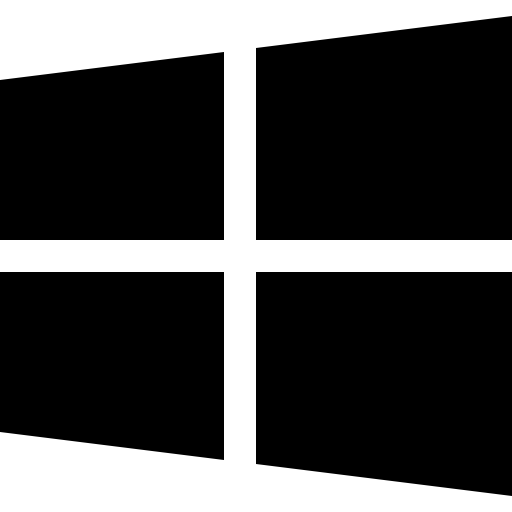इसराइल फिलिस्तीन संघर्ष वैश्विक राजनीति के सबसे जटिल और लंबे समय से चल रहे मुद्दों में से एक है, जो वर्तमान मामलों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। उदाहरण के लिए, इस संघर्ष ने मध्य पूर्व में अंतरराष्ट्रीय संबंधों को आकार दिया है और वैश्विक नीति चर्चाओं को प्रभावित किया है, जिससे यह IAS उम्मीदवारों और समकालीन मुद्दों को समझने में रुचि रखने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण विषय बन गया है।
क्या आप जानते हैं?
इसराइल मुद्दे की जटिलताओं को समझने के लिए अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर अपडेट रहना आवश्यक है, जैसे IAS परीक्षा की तैयारी के लिए वर्तमान मामलों के बारे में जानकारी रखना जरूरी है। MalukaIAS Acadamy के वर्तमान मामलों के संसाधन आपकी परीक्षा में सफलता के लिए मदद कर सकते हैं।
जैसे इसराइल-फिलिस्तीन संघर्ष को समझने के लिए इतिहास और राजनीति में एक मजबूत आधार की आवश्यकता होती है, IAS/PCS परीक्षाओं में सफलता के लिए गहन तैयारी आवश्यक है। मलुका IAS अकादमी का GS Foundation Advance Batch 2025 आपकी सफलता के लिए आवश्यक कोचिंग प्रदान करता है।
ज्योतिषीय मुद्दों का विश्लेषण करने वाले और IAS उम्मीदवार दोनों को प्रभावी तैयारी की रणनीतियों की आवश्यकता होती है। परीक्षाओं के लिए निरंतर अभ्यास आवश्यक है। अपने कौशल को सुधारने के लिए Maluka IAS अकादमी की Prelims and Mains test series का पता लगाएं।
अंतरराष्ट्रीय संबंधों में बदलावों की जानकारी रखना बेहद ज़रूरी है, ठीक वैसे ही जैसे IAS परीक्षा पैटर्न से अपडेट रहना। IAS परीक्षाओं में सफलता के लिए समसामयिक घटनाओं की जानकारी आवश्यक होती है। मलूका IAS एकेडमी के current affairs के संसाधन छात्रों को संपूर्ण परीक्षा की तैयारी में मदद करते हैं।
जब लोग इसराइल मुद्दे के प्रभावों पर चर्चा करते हैं, तो IAS/PCS उम्मीदवारों को अपनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। मलुका IAS अकादमी की Punjab PCS Online Coaching आपको इन्हें पार करने में मदद कर सकती है।
इसराइल फिलिस्तीन संघर्ष: इज़राइली राज्य के गठन के विभिन्न चरण
इज़राइल राज्य का गठन एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया थी, जिसमें कई अलग-अलग चरण शामिल थे, प्रत्येक चरण महत्वपूर्ण घटनाओं और चुनौतियों से चिह्नित था। यहाँ प्रमुख चरणों का विवरण है:
1. प्रारंभिक ज़ायोनी आंदोलन और यहूदी राष्ट्रवाद का उदय (19वीं सदी के अंत - 20वीं सदी की शुरुआत):
- विरोधी-यहूदीवाद और उत्पीड़न: यूरोप में, खासकर रूस में बढ़ते विरोधी-यहूदीवाद ने ज़ायोनीवाद के विकास को प्रेरित किया, जो फिलिस्तीन में एक यहूदी मातृभूमि की वकालत करने वाला एक आंदोलन था।
- प्रारंभिक ज़ायोनी संगठन: होवेव ज़ायोन (ज़ायोन के प्रेमी) और विश्व ज़ायोनी संगठन (डब्ल्यूज़ीओ) जैसे संगठन स्थापित किए गए, जो फिलिस्तीन में यहूदी बसावट को बढ़ावा देते थे।
- पहली अलीया (प्रवास): 1880 के दशक में शुरू होकर, फिलिस्तीन में यहूदी प्रवासियों की पहली लहर ने कृषि बस्तियाँ स्थापित कीं और इस क्षेत्र में यहूदी उपस्थिति की नींव रखी।
2. फिलिस्तीन के लिए ब्रिटिश जनादेश (1920-1948):
- प्रथम विश्व युद्ध के बाद: प्रथम विश्व युद्ध के बाद, ब्रिटिश साम्राज्य ने राष्ट्र संघ के जनादेश के तहत फिलिस्तीन पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया।
- बढ़ती यहूदी प्रवास: इस अवधि के दौरान फिलिस्तीन में महत्वपूर्ण यहूदी प्रवास हुआ, जिससे मौजूदा अरब आबादी के साथ बढ़ता तनाव हुआ।
- अरब प्रतिरोध और अशांति: यहूदी बस्तियों और ब्रिटिश शासन का अरब विरोध तेज हो गया, जिसका परिणाम विभिन्न विद्रोह और संघर्षों में हुआ।
3. द्वितीय विश्व युद्ध और प्रलय:
- प्रलय का प्रभाव: प्रलय की भयावहता ने एक सुरक्षित यहूदी मातृभूमि स्थापित करने की तात्कालिकता को रेखांकित किया और ज़ायोनी आंदोलन के प्रयासों को तेज कर दिया।
- ज़ायोनीवाद के लिए बढ़ता अंतरराष्ट्रीय समर्थन: प्रलय के बाद, एक यहूदी राज्य के निर्माण के लिए वैश्विक स्तर पर बढ़ता समर्थन था, जिसके कारण संयुक्त राष्ट्र विभाजन योजना को अपनाया गया।
4. संयुक्त राष्ट्र विभाजन योजना और 1948 का अरब-इज़रायली युद्ध:
- संयुक्त राष्ट्र विभाजन योजना (1947): संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन को दो राज्यों, एक यहूदी और एक अरब में विभाजित करने की योजना अपनाई।
- अरब अस्वीकृति और युद्ध: अरब राज्यों ने योजना को अस्वीकार कर दिया, जिसके कारण 1948 का अरब-इज़रायली युद्ध हुआ, जिसके परिणामस्वरूप इज़राइल की जीत हुई और लाखों फिलिस्तीनी विस्थापित हो गए।
- स्वतंत्रता की घोषणा: 14 मई, 1948 को, इज़राइल ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की, जो इज़राइल राज्य के जन्म को चिह्नित करता है।
5. राज्य के प्रारंभिक वर्ष (1948-1967):
- राज्य के एकीकरण: अपने शुरुआती वर्षों में, इज़राइल को पड़ोसी अरब राज्यों के साथ चल रहे संघर्षों सहित कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा।
- विकास और विकास: चुनौतियों के बावजूद, इज़राइल ने आर्थिक विकास, शिक्षा और बुनियादी ढांचे में उल्लेखनीय प्रगति की।
6. छह दिवसीय युद्ध और इज़राइली क्षेत्र का विस्तार (1967):
- छह दिवसीय युद्ध: इज़राइल के लिए एक निर्णायक जीत, जिसके परिणामस्वरूप सिनाई प्रायद्वीप, वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी और गोलान हाइट्स पर कब्जा हुआ।
- प्रादेशिक विवाद और कब्जा: इज़राइली क्षेत्र का विस्तार जारी प्रादेशिक विवादों और फिलिस्तीनी क्षेत्रों के कब्जे को जन्म देता है।
7. ओस्लो समझौते और शांति की खोज (1990 के दशक-वर्तमान):
- ओस्लो समझौते (1993): इज़राइल और फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन (पीएलओ) के बीच एक ऐतिहासिक समझौता, जिसका उद्देश्य दो-राज्य समाधान है।
- जारी संघर्ष और वार्ता: ओस्लो समझौतों के माध्यम से की गई प्रगति के बावजूद, शांति प्रक्रिया को चल रहे संघर्षों और असफलताओं का सामना करना पड़ा है।
- वर्तमान स्थिति: इज़राइली-फिलिस्तीनी संघर्ष अनसुलझा है, जिसमें शांति की चल रही खोज को प्रभावित करने वाले कई जटिल मुद्दे हैं।
अरब-इज़राइल संघर्ष के कारण:
अरब-इज़राइल संघर्ष एक गहरा जटिल और बहुआयामी मुद्दा है जिसकी जड़ें एक सदी से भी अधिक समय से फैली हुई हैं। यह केवल भूमि पर एक संघर्ष नहीं है, बल्कि ऐतिहासिक शिकायतों, राजनीतिक आकांक्षाओं, धार्मिक विश्वासों और पहचान संघर्षों का एक जटिल जाल है। इस स्थायी संघर्ष को बढ़ावा देने वाले कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार हैं:
1. ऐतिहासिक भूमि दावे और राष्ट्रीय पहचान:
- फिलिस्तीनी आख्यान: फिलिस्तीनी फिलिस्तीन की भूमि के लिए ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों का दावा करते हैं, यहूदी बस्तियों को एक औपनिवेशिक परियोजना के रूप में देखते हैं जिसने उन्हें बेदखल कर दिया।
- ज़ायोनी आख्यान: ज़ायोनी, एक यहूदी मातृभूमि की वकालत करते हुए, तर्क देते हैं कि भूमि के लिए ऐतिहासिक और धार्मिक संबंध, यूरोपीय उत्पीड़न के साथ मिलकर, फिलिस्तीन में एक राज्य के लिए उनके दावे को सही ठहराते हैं।
2. 1948 का युद्ध और फिलिस्तीनी शरणार्थी संकट:
- संयुक्त राष्ट्र विभाजन योजना: 1947 में संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव ने फिलिस्तीन को दो राज्यों में विभाजित करने का प्रस्ताव दिया, एक यहूदी और एक अरब। अरब नेताओं ने योजना को अस्वीकार कर दिया, जिससे युद्ध छिड़ गया।
- फिलिस्तीनियों का विस्थापन: 1948 के युद्ध के परिणामस्वरूप लाखों फिलिस्तीनी विस्थापित हो गए, जो शरणार्थी बन गए, और अपनी भूमि गंवा बैठे।
- वापसी का अधिकार: फिलिस्तीनी शरणार्थियों और उनके वंशजों ने इज़राइल में अपने पूर्व घरों में लौटने के अधिकार की मांग जारी रखी है, जो शांति वार्ता में एक प्रमुख बाधा है।
3. कब्जा और बस्तियाँ:
- छह दिवसीय युद्ध (1967): छह दिवसीय युद्ध में इज़राइल की जीत के कारण वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी, पूर्वी यरूशलेम और गोलान हाइट्स पर उसका नियंत्रण हो गया।
- बस्तियाँ: इज़राइल ने कब्जे वाले क्षेत्रों में बस्तियाँ बनाना शुरू कर दिया, जिन्हें फिलिस्तीनी अवैध और एक व्यवहार्य स्वतंत्र राज्य के लिए एक बाधा मानते हैं। इन बस्तियों को शांति के लिए एक बड़ी बाधा के रूप में देखा जाता है।
4. सुरक्षा संबंधी चिंताएँ और राजनीतिक विभाजन:
- आतंकवाद और सुरक्षा: इज़राइल ने कई आतंकवादी हमलों का सामना किया है, जिससे सुरक्षा संबंधी चिंताएँ बढ़ी हैं और कब्जे वाले क्षेत्रों पर नियंत्रण बनाए रखने की इच्छा है।
- आंतरिक विभाजन: फिलिस्तीनी और इज़राइली दोनों समाज गहराई से विभाजित हैं, जिससे शांति समझौते पर सहमति बनाना मुश्किल हो जाता है।
- धार्मिक और वैचारिक मतभेद: इज़राइलियों और फिलिस्तीनियों के बीच धार्मिक और वैचारिक मतभेद, खासकर यरूशलेम की स्थिति को लेकर, संघर्ष को और जटिल बनाते हैं।
5. अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी और वैश्विक राजनीति:
- अंतरराष्ट्रीय समर्थन: दोनों पक्षों को अंतरराष्ट्रीय समर्थन प्राप्त हुआ है, कुछ देश इज़राइल को मान्यता देते हैं और अन्य फिलिस्तीनी कारण का समर्थन करते हैं।
- महान शक्ति का प्रभाव: संघर्ष अक्सर वैश्विक राजनीति से जुड़ा रहा है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य महाशक्तियाँ शांति वार्ता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
इज़राइल फिलिस्तीन संघर्ष पर भारत का रुख:
इज़राइल-फिलिस्तीन संघर्ष पर भारत का रुख जटिल और सूक्ष्म है, जो ऐतिहासिक संबंधों, राजनीतिक वास्तविकताओं और घरेलू विचारों के बीच सावधानीपूर्वक संतुलन को दर्शाता है। यहाँ प्रमुख पहलुओं का विवरण है:
ऐतिहासिक संबंध:
- फिलिस्तीनी स्वशासन के लिए भारत का समर्थन: भारत ऐतिहासिक रूप से फिलिस्तीनी अधिकारों और दो-राज्य समाधान का एक मजबूत समर्थक रहा है। यह भारत के ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ स्वतंत्रता के संघर्ष से उपजा है, जो मुक्ति आंदोलनों के साथ एक मजबूत एकजुटता बनाता है।
- इज़राइल की मान्यता: भारत ने 1950 में इज़राइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए, जो ऐसा करने वाले पहले गैर-अरब देशों में से एक बन गया। यह उपनिवेशवाद विरोधी संघर्षों का सामना करने के साझा अनुभव और आर्थिक और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने की इच्छा से प्रेरित था।
राजनीतिक वास्तविकताएँ:
- इज़राइल के साथ रणनीतिक साझेदारी: हाल के वर्षों में, भारत और इज़राइल ने रक्षा सहयोग, प्रौद्योगिकी साझाकरण और खुफिया आदान-प्रदान को शामिल करते हुए एक मजबूत रणनीतिक साझेदारी विकसित की है। यह रिश्ता आतंकवाद का मुकाबला करने, ऊर्जा आपूर्ति को सुरक्षित करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के पारस्परिक हितों से प्रेरित है।
- अरब राज्यों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना: भारत सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे प्रमुख तेल आपूर्तिकर्ता सहित कई अरब देशों के साथ भी मजबूत संबंध बनाए रखता है। भारत इज़राइल के साथ अपने संबंधों को संतुलित करने का प्रयास करता है जबकि अपने अरब भागीदारों को अलग नहीं करता है।
घरेलू विचार:
- महत्वपूर्ण मुस्लिम आबादी: भारत में एक बड़ी मुस्लिम आबादी है, और इज़राइल के प्रति किसी भी कथित पूर्वाग्रह को राजनीतिक रूप से संवेदनशील माना जा सकता है।
- गैर-संरेखण नीति: भारत की पारंपरिक विदेश नीति गैर-संरेखण पर आधारित रही है, किसी विशेष गुट के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता से बचना। यह सिद्धांत भारत को अंतरराष्ट्रीय विवादों में पक्ष लेने से बचने के लिए बाध्य करता है।
भारत का वर्तमान दृष्टिकोण:
- दो-राज्य समाधान का समर्थन करना: भारत एक शांतिपूर्ण समाधान की वकालत करना जारी रखता है जो दो-राज्य समाधान पर आधारित हो, जिसमें इज़राइल और फिलिस्तीन दोनों शांति और सुरक्षा में एक साथ रहें।
- संवाद और कूटनीति पर ध्यान केंद्रित: भारत का मानना है कि एक स्थायी समाधान केवल बातचीत और कूटनीति के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, दोनों पक्षों को सार्थक वार्ता में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
- फिलिस्तीन को मानवीय सहायता: भारत फिलिस्तीन को मानवीय सहायता प्रदान करता है, राहत प्रयासों और विकास परियोजनाओं का समर्थन करता है।
चुनौतियाँ:
- फिलिस्तीनियों के लिए ऐतिहासिक समर्थन को इज़राइल के साथ रणनीतिक संबंधों के साथ संतुलित करना: भारत एक नाजुक संतुलन का सामना करता है, फिलिस्तीनी कारण के प्रति अपनी लंबी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की कोशिश करता है, जबकि इज़राइल के साथ अपने महत्वपूर्ण संबंधों को खतरे में नहीं डालता है।
- क्षेत्र में तनाव बढ़ना: क्षेत्र में हिंसा के हालिया बढ़ने से भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि वह अपनी शांति और कूटनीति के सिद्धांतों को बनाए रखते हुए अपनी तटस्थता बनाए रखना चाहता है।
संभावित समाधान:
- दो-राज्य समाधान: सबसे व्यापक रूप से समर्थित: यह संयुक्त राष्ट्र, प्रमुख विश्व शक्तियों और कई अंतरराष्ट्रीय संगठनों द्वारा समर्थित सबसे व्यापक रूप से समर्थित समाधान बना हुआ है।
- एक-राज्य समाधान: एक राष्ट्र जहाँ यहूदियों और फिलिस्तीनियों दोनों को समान अधिकार प्राप्त हों।
- संयुक्त राष्ट्र की भागीदारी: दोनों पक्षों पर मजबूत शांतिरक्षा बलों और अंतरराष्ट्रीय दबाव सहित संयुक्त राष्ट्र की बढ़ती भागीदारी, प्रगति के लिए एक उत्प्रेरक हो सकती है।
- अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण: युद्ध अपराधों और मानवाधिकारों के उल्लंघन की जाँच करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण स्थापित करने से जवाबदेही को संबोधित करने और संभावित रूप से सुलह का मार्ग प्रशस्त करने में मदद मिल सकती है।
- आर्थिक प्रोत्साहन: दोनों पक्षों को समझौता करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सहायता और निवेश का उपयोग किया जा सकता है।
- आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित: इज़राइलियों और फिलिस्तीनियों दोनों के लिए आर्थिक संभावनाओं में सुधार से शांति और सहयोग में साझा रुचि पैदा हो सकती है।
निष्कर्ष:
अरब-इज़राइल संघर्ष एक गहरा जटिल और बहुआयामी मुद्दा है जिसका कोई आसान समाधान नहीं है। ऐतिहासिक शिकायतों, सुरक्षा संबंधी चिंताओं, प्रादेशिक विवादों और राजनीतिक विभाजनों का समाधान करने के लिए सभी संबंधित पक्षों से महत्वपूर्ण समझौता और समझ की आवश्यकता होगी। शांतिपूर्ण समाधान की खोज एक लंबी और कठिन प्रक्रिया है।

-1721391937657.png)