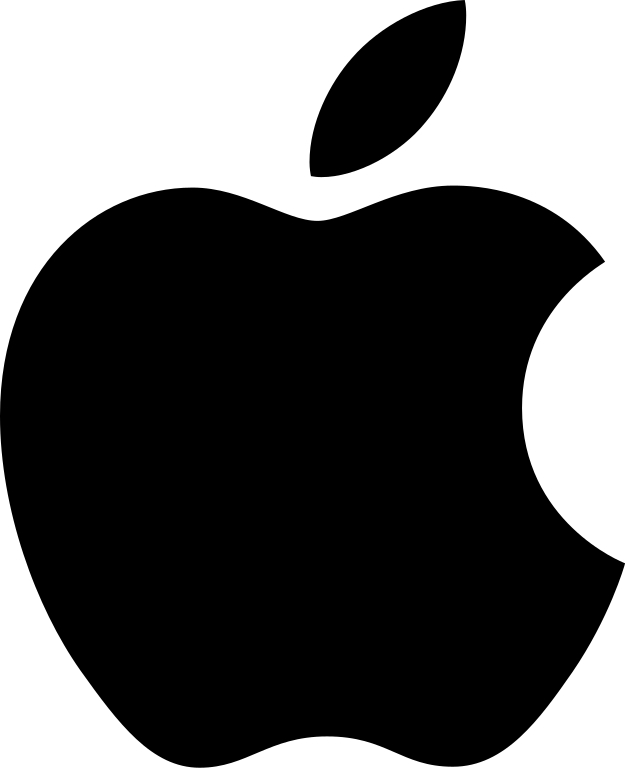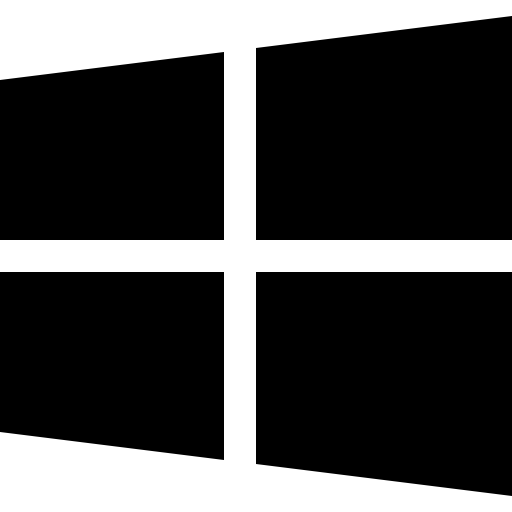महात्मा गांधी ने एक बार कहा था, "जब कोई महिला रात में स्वतंत्र रूप से चल सकेगी, तब भारत वास्तव में स्वतंत्र होगा।" कोलकाता में एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ हाल ही में हुए बलात्कार और हत्या ने महिलाओं की सुरक्षा के बारे में चिंताओं को फिर से जगा दिया है, जो निर्भया मामले में लोगों के आक्रोश की याद दिलाता है। तकनीकी प्रगति और शहरीकरण के बावजूद, भारत में अभी भी महिलाओं के खिलाफ बड़े पैमाने पर हिंसा और भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें प्रतिदिन लगभग 88 बलात्कार की रिपोर्ट की जाती है और कई मामले रिपोर्ट नहीं किए जाते हैं। यह त्रासदी महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमारे सांस्कृतिक मूल्यों की विफलता को उजागर करती है, जो समाज की आधारशिला हैं।
क्या आप जानते हैं?
महिला सुरक्षा से जुड़े कानूनों की जानकारी IAS परीक्षाओं के Current Affairs notes का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मलूका IAS अकादमी के संसाधन छात्रों को महिलाओं की सुरक्षा और उनसे जुड़े कानूनों के बारे में अद्यतन रखने में मदद करते हैं, जो प्रीलिम्स और मेन्स दोनों के लिए आवश्यक हैं।
जैसे महिलाओं की सुरक्षा के लिए सतर्कता आवश्यक है, वैसे ही IAS की तैयारी के लिए रणनीतिक दृष्टिकोण की जरूरत होती है। मलूका IAS अकादमी का GS Foundation Advance Batch 2025, समाज के महत्वपूर्ण मुद्दों जैसे महिलाओं के अधिकार और सुरक्षा पर गहराई से शिक्षण प्रदान करता है।
महिला सुरक्षा जैसे मुद्दे न केवल IAS परीक्षाओं में आते हैं बल्कि समाज की चुनौतियों को समझने का भी हिस्सा हैं। मलूका IAS अकादमी का Prelims and Mains Test Series छात्रों को इस तरह के महत्वपूर्ण विषयों पर प्रश्नों को प्रभावी ढंग से हल करने का अभ्यास कराती है।
महिला सुरक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जो IAS और PCS परीक्षाओं में पब्लिक पॉलिसी चर्चा में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मलूका IAS अकादमी के Punjab PCS Online के माध्यम से, आप जान सकते हैं कि महिलाओं के अधिकार और सुरक्षा से जुड़े कानून किस तरह सार्वजनिक प्रशासन को आकार देते हैं।
महिला सुरक्षा नीतियों की समझ IAS उम्मीदवारों को सामाजिक मुद्दों पर एक व्यापक दृष्टिकोण देती है। Maluka IAS Academy का गहन करंट अफेयर्स सामग्री, सुरक्षा नीतियों पर समझ विकसित करने में मदद करती है, जिससे आप परीक्षा में व्यापक समझ के साथ जा सकते हैं।
भारत में महिलाओं की सुरक्षा संबंधी चिंताएँ
भारत में महिला सुरक्षा के मुद्दे: महिलाओं को देवी के रूप में पूजने के बावजूद, भारत में महिला सुरक्षा के गंभीर मुद्दे हैं, जिनमें बलात्कार, छेड़छाड़, घरेलू हिंसा, मारपीट, बाल विवाह और दहेज के मामले शामिल हैं। पिछले एक दशक में महिलाओं की भेद्यता में काफी वृद्धि हुई है।
भारत में अपर्याप्त महिला सुरक्षा के कारण
- पितृसत्ता: गहरी जड़ें जमाए बैठी पितृसत्तात्मक मान्यताएं, जैसे "लड़का है, गलती हो जाती है" मानसिकता, पुरुष श्रेष्ठता और महिलाओं के खिलाफ हिंसा को सामान्य बनाती हैं।
- महिलाओं का वस्तुकरण: मीडिया और मनोरंजन में अक्सर महिलाओं को वस्तु के रूप में चित्रित किया जाता है, जिससे उत्पीड़न और हिंसा में वृद्धि होती है।
- सांस्कृतिक कलंक: यौन हिंसा से जुड़े कलंक के कारण उत्पीड़न की रिपोर्ट कम दर्ज की जाती है और उत्पीड़न की रिपोर्ट करने वाली महिलाओं के खिलाफ सामाजिक प्रतिक्रिया होती है।
- आर्थिक निर्भरता: परिवार के पुरुष सदस्यों पर अत्यधिक आर्थिक निर्भरता महिलाओं की भेद्यता को बढ़ाती है तथा दुर्व्यवहार से बचने की उनकी क्षमता को सीमित करती है।
- जागरूकता का अभाव: कई महिलाएं घरेलू हिंसा अधिनियम और यौन उत्पीड़न अधिनियम जैसे कानूनी संरक्षणों से अनभिज्ञ हैं, जिससे दुर्व्यवहार का चक्र चलता रहता है।
- अपर्याप्त सार्वजनिक सुरक्षा: अपर्याप्त प्रकाश व्यवस्था और सुरक्षित परिवहन की कमी जैसी खराब सार्वजनिक अवसंरचना के कारण महिलाओं में अपराध की संभावना बढ़ जाती है।
एनसीआरबी रिपोर्ट 2023 महिलाओं के खिलाफ अपराध से संबंधित आंकड़े
- समग्र वृद्धि: एनसीआरबी रिपोर्ट 2023 महिलाओं के खिलाफ अपराधों में 4% की वृद्धि दर्शाती है, जो 2021 में 4,28,278 मामलों से बढ़कर 2022 में 4,45,256 मामले हो जाएंगे। प्रति लाख महिलाओं पर अपराध दर 64.5 से बढ़कर 66.4 हो गई।
- अपराध के प्रकार:
- पति या रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता: 31.4%
- अपहरण और भगा ले जाना: 19.2%
- शील भंग करने के लिए आक्रमण: 18.7%
- बलात्कार: 7.1%
- महिला सुरक्षा सूचकांक: महिला, शांति और सुरक्षा सूचकांक 2023 में भारत 0.58 स्कोर के साथ 177 देशों में से 128वें स्थान पर है, जो इसे महिला सुरक्षा के लिए चौथे क्विंटल में रखता है।
- राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5): राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5) की रिपोर्ट बताती है कि भारत में 15-49 वर्ष की आयु की लगभग 30% महिलाओं ने शारीरिक, यौन या घरेलू हिंसा का अनुभव किया है।
महिलाओं के विरुद्ध अपराध रोकने के लिए सरकारी पहल
कानूनी संरक्षण
बाल हिंसा के खिलाफ
- बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006
- किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015
- बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम
- यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012
महिलाओं को अपमानित करने के खिलाफ
- महिलाओं का अशिष्ट चित्रण (निषेध) अधिनियम, 1986
यौन अपराधों के विरुद्ध
- कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013।
- यौन अपराधों के विरुद्ध प्रभावी कानूनी निवारण के लिए आपराधिक कानून (संशोधन), अधिनियम 2013।
- आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2018 में 12 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं के साथ बलात्कार के लिए मृत्युदंड सहित और भी कठोर दंडात्मक प्रावधान किए गए हैं।
घरेलू हिंसा के खिलाफ
- दहेज निषेध अधिनियम, 1961
- घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005।
केन्द्र सरकार की पहल
- निर्भया फंड: महिलाओं की सुरक्षा पर केंद्रित परियोजनाओं के लिए सरकार द्वारा स्थापित।
- यौन अपराधों के लिए जांच ट्रैकिंग प्रणाली: आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम 2018 के अनुसार यौन उत्पीड़न के मामलों में समयबद्ध जांच की निगरानी और सुनिश्चित करने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा शुरू की गई।
- यौन अपराधियों पर राष्ट्रीय डेटाबेस (NDSO): कानून प्रवर्तन एजेंसियों को यौन अपराधियों पर नज़र रखने और उनकी जांच करने में मदद करने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक डेटाबेस, जिसमें 5 लाख से अधिक अपराधियों का डेटा शामिल है।
- साइबर अपराध पोर्टल: ऑनलाइन अश्लील सामग्री की रिपोर्ट करने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक मंच, जिसे विभिन्न राज्यों में साइबर अपराध फोरेंसिक प्रयोगशालाओं द्वारा समर्थित किया गया है।
- वन स्टॉप सेंटर: हिंसा से प्रभावित महिलाओं को एकीकृत समर्थन और सहायता प्रदान करने की एक योजना।
- महिला हेल्पलाइन का सार्वभौमिकरण: हिंसा से प्रभावित महिलाओं को आपातकालीन और गैर-आपातकालीन सहायता प्रदान करने के लिए 24 घंटे की हेल्पलाइन शुरू की गई।
राज्य सरकार और अन्य पहल
- मेरी सहेली पहल: समर्पित महिला अधिकारियों के साथ महिला ट्रेन यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रेलवे सुरक्षा बल द्वारा शुरू की गई
- शक्ति आपराधिक कानून (महाराष्ट्र संशोधन) अधिनियम: बलात्कार और सामूहिक बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों के लिए मौत की सजा को मंजूरी देने वाला महाराष्ट्र विधानसभा कानून
- मिशन शक्ति: महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने और हिंसा और शोषण को कम करने के लिए यूपी सरकार द्वारा शुरू किया गया
- पुलिस पिंक बूथ: महिलाओं की शिकायतों के समाधान के लिए समर्पित बूथ उपलब्ध कराने की दिल्ली सरकार की पहल
- ऑनलाइन आंदोलन और अभियान: जागरूकता बढ़ाने और महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न को रोकने के लिए #CallItOut, #ItsNotOK, और #MeToo जैसी पहल
कानूनी और नीतिगत पहल के बावजूद महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने में चुनौतियाँ
- विलंबित न्याय: लंबी कानूनी प्रक्रिया और यौन अपराधियों के लिए नरम दंड से कानून प्रवर्तन में जनता का विश्वास खत्म हो जाता है।
- ढीली दोषसिद्धि प्रक्रिया: 39% अधिकारियों का मानना है कि लिंग आधारित हिंसा की शिकायतें निराधार हैं। धीमी गति से एफआईआर दर्ज करना, समयबद्ध जांच और खराब फोरेंसिक साक्ष्य संग्रह यौन उत्पीड़न के मामलों में दोषसिद्धि में देरी करते हैं।
- आधे-अधूरे मन से कार्यान्वयन: सर्वोच्च न्यायालय ने महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्यस्थल सुनिश्चित करने में विफल रहने के लिए अधिकारियों की आलोचना की है तथा कहा है कि यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013 का कार्यान्वयन अपर्याप्त रहा है।
- सार्वजनिक धन का अप्रभावी उपयोग: 2013 से 2022 तक निर्भया फंड में 100% वृद्धि के बावजूद, आवंटित धनराशि का आधे से भी कम उपयोग किया गया है।
महिलाओं के प्रति प्रचलित दृष्टिकोण और अपराध के निहितार्थ
- कार्यबल निवारण: महिलाओं के विरुद्ध अपराध भारत में महिलाओं की कार्यबल में कम भागीदारी का कारण हैं।
- अंधराष्ट्रीय पारिवारिक दृष्टिकोण: कई पुरुष अपने परिवार में महिलाओं को वित्तीय या सामाजिक स्वतंत्रता प्राप्त करने से हतोत्साहित करते हैं।
- सामाजिक दृष्टिकोण और अपराध: बालिकाओं के विरुद्ध अपराधों से उत्पन्न लैंगिक असंतुलन के कारण अपहरण और विवाह के लिए अपहरण जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं।
- स्वास्थ्य परिणाम: यौन हिंसा से गंभीर शारीरिक चोटें और दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जिनमें दीर्घकालिक दर्द, प्रजनन संबंधी समस्याएं और यौन संचारित रोगों का जोखिम बढ़ जाना शामिल है।
- परिवारों पर प्रभाव: माताओं के विरुद्ध हिंसा देखने वाले बच्चों को भावनात्मक, व्यवहारिक समस्याओं का खतरा होता है, तथा वे दुर्व्यवहार के चक्र को जारी रख सकते हैं।
आगे की राह
- पुलिस सुधार: लिंग आधारित भर्ती और प्रशिक्षण, महिला पुलिस थानों की स्थापना, तथा महिला पुलिस स्वयंसेवकों की नियुक्ति पर ध्यान केन्द्रित किया जाए।
- न्यायिक सुधार: न्यायमूर्ति वर्मा समिति की सिफारिश के अनुसार फास्ट-ट्रैक अदालतें स्थापित की जाएं, बलात्कार जैसे गंभीर अपराधों के लिए दंड बढ़ाया जाए तथा न्यायपालिका में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाए।
- प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण: जांच, अभियोजन और चिकित्सा अधिकारियों के प्रशिक्षण में सुधार करना, लिंग-संवेदनशील प्रथाओं को बढ़ावा देना, तथा आपराधिक मामलों में आघात-सूचित दृष्टिकोण सुनिश्चित करना।
- बलात्कार संकट केंद्र: ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और ब्रिटेन जैसे केन्द्रों की स्थापना करना, जो बलात्कार पीड़ितों को चिकित्सा सहायता, परामर्श और वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- मीडिया संवेदनशीलता: यह सुनिश्चित करें कि मीडिया बलात्कार पीड़ितों की पहचान उजागर न करे तथा उन मामलों को उजागर करे जिनमें अपराधियों को दोषी ठहराया गया है, ताकि भविष्य में होने वाले अपराधों को रोका जा सके।
- नागरिक समाज की भागीदारी: अपराधों से निपटने और कानून प्रवर्तन में सहयोग देने के लिए नागरिक समाज की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करें।

-1721391937657.png)