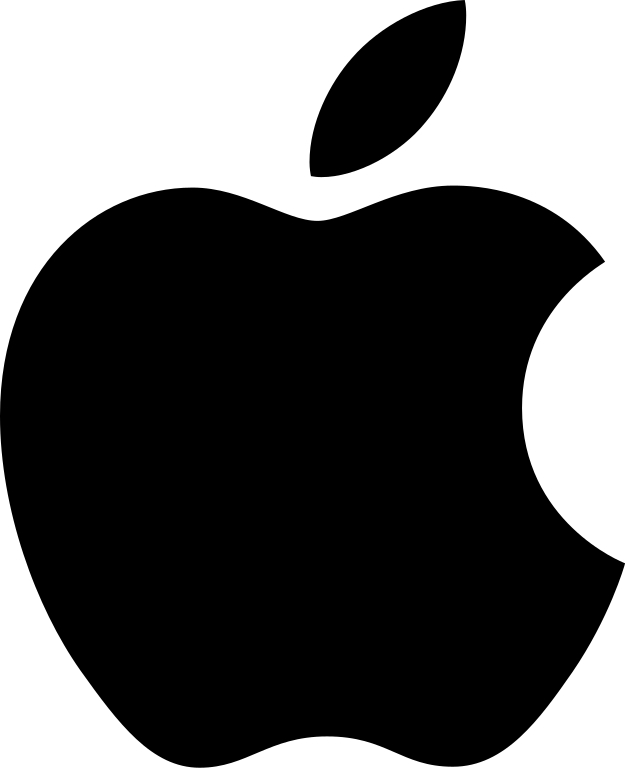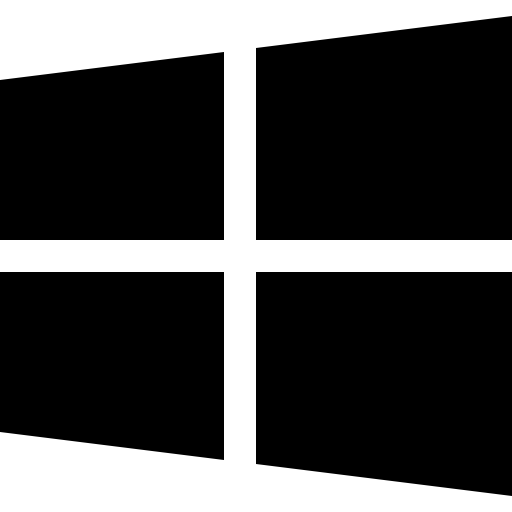भारत में दल-बदल कानून का उद्देश्य राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित करना और निर्वाचित प्रतिनिधियों को दल बदलने से रोकना है। इसे 1985 में संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत लागू किया गया था। इस कानून का उद्देश्य राजनीतिक भ्रष्टाचार को रोकना और लोकतंत्र की गरिमा बनाए रखना है।
दल-बदल कानून के प्रमुख प्रावधान
-
अयोग्यता के आधार:
- स्वैच्छिक पार्टी छोड़ना: यदि कोई सदस्य उस पार्टी की सदस्यता छोड़ देता है, जिसके टिकट पर वह निर्वाचित हुआ है।
- पार्टी निर्देशों के विरुद्ध मतदान: यदि कोई विधायक पार्टी के निर्देशों के विपरीत मतदान करता है या मतदान से अनुपस्थित रहता है।
-
अयोग्यता के अपवाद:
- राजनीतिक दलों का विलय: यदि किसी दल के दो-तिहाई सदस्य किसी अन्य दल में विलय का समर्थन करते हैं, तो इसे दल-बदल नहीं माना जाएगा।
- स्पीकर/उपाध्यक्ष का चुनाव: स्पीकर या उपाध्यक्ष चुने जाने वाले सदस्य अपनी पार्टी छोड़ सकते हैं और कार्यकाल समाप्त होने के बाद फिर से जुड़ सकते हैं।
-
अयोग्यता का निर्णय:
- लोकसभा के स्पीकर या विधान सभा के अध्यक्ष अयोग्यता के मामलों का निर्णय लेते हैं।
दल-बदल कानून का महत्व
-
राजनीतिक स्थिरता:
- निर्वाचित प्रतिनिधियों को व्यक्तिगत लाभ के लिए दल बदलने से रोकता है।
-
जवाबदेही:
- विधायकों को पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों का पालन करने के लिए प्रेरित करता है।
-
भ्रष्टाचार पर अंकुश:
- राजनीति में रिश्वतखोरी और दल-बदल की संभावना को कम करता है।
-
पार्टी अनुशासन:
- पार्टी में आंतरिक अनुशासन और एकता को बढ़ावा देता है।
चुनौतियां और आलोचनाएं
-
स्पीकर की पक्षपातपूर्ण भूमिका:
- आलोचकों का मानना है कि स्पीकर पार्टी सदस्य होने के कारण निष्पक्षता से काम नहीं करते।
-
स्वतंत्रता पर अंकुश:
- विधायकों को स्वतंत्र रूप से राय व्यक्त करने की स्वतंत्रता कम हो जाती है।
-
अपवादों का दुरुपयोग:
- विलय का प्रावधान अक्सर कानून को दरकिनार करने के लिए उपयोग किया जाता है।
-
न्यायिक समीक्षा में देरी:
- स्पीकर के निर्णयों को अदालत में चुनौती दी जा सकती है, लेकिन प्रक्रिया में देरी होती है।
महत्वपूर्ण निर्णय
-
किहोटो होलोहोन केस (1992):
- सुप्रीम कोर्ट ने दल-बदल कानून की वैधता को बरकरार रखा, लेकिन स्पीकर के फैसलों की न्यायिक समीक्षा की अनुमति दी।
-
मणिपुर केस (2020):
- अदालत ने अयोग्यता याचिकाओं पर समयबद्ध निर्णय की आवश्यकता पर जोर दिया।
प्रस्तावित सुधार
-
स्वतंत्र ट्रिब्यूनल:
- अयोग्यता के मामलों को निर्णय के लिए स्पीकर की बजाय स्वतंत्र ट्रिब्यूनल को सौंपना।
-
स्पष्ट समय-सीमा:
- अयोग्यता मामलों पर निर्णय के लिए निश्चित समय-सीमा निर्धारित करना।
-
लोकतांत्रिक सिद्धांतों को मजबूत करना:
- विधायकों को महत्वपूर्ण मुद्दों पर स्वतंत्र रूप से विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता देना।
निष्कर्ष
दल-बदल कानून भारत के लोकतंत्र में राजनीतिक स्थिरता और अनुशासन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि, इसके सामने आने वाली चुनौतियों को दूर करने के लिए सुधार आवश्यक हैं, ताकि यह लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर किए बिना अपने उद्देश्य को प्रभावी ढंग से पूरा कर सके।

-1721391937657.png)